पर्युषण महापर्व - इतिहास के झरोखे से
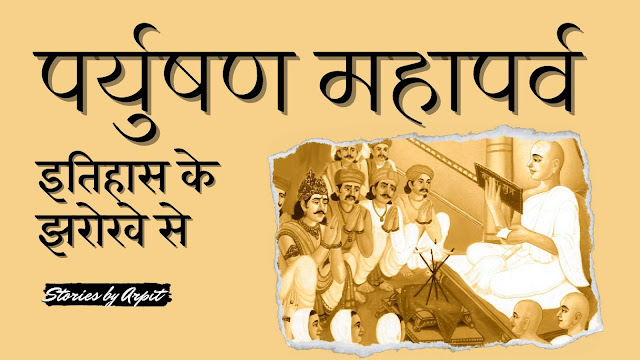 |
जैन दर्शन में पर्वों को लौकिक पर्व और आध्यात्मिक पर्व में विभाजित किया गया है. पर्युषण महापर्व की गणना आध्यात्मिक पर्व के रूप में की गई है और इसे सबसे पवित्र पर्व का दर्जा दिया गया है. आगम छेदसूत्र - श्री आयारदशा (दशाश्रुतस्कंध) एवं श्री निशीथ सूत्र आदि आगम ग्रन्थों में पर्युषण के मूल प्राकृत शब्द रूप "पज्जोसवण" का प्रयोग हुआ है.
वर्तमान समय में, पर्युषण पर्व को श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संप्रदाय के तपागच्छ और खरतरगच्छ में श्रावण वदी १२ से भाद्रपद शुक्ल ४ तक मनाया जाता है और मूर्तिपूजक संप्रदाय के अंचलगच्छ, पार्श्वचंद्रगच्छ एवं अमूर्तिपूजक सम्प्रदाय के स्थानकवासी और तेरापंथ में श्रावण वदी १३ से भाद्रपद शुक्ल ५ तक मनाया जाता है. पर्युषण पर्व के ८वे दिन, अर्थात् सवंत्सरी की आराधना द्वारा, पुरे वर्ष में किये गए पापो का परायश्चित करने के साथ-साथ विश्व के समस्त जीवो से क्षमायाचना करना यह पर्व का मुख्य अंग है. परन्तु, आज मुख्यत्व: जैनो को इस महापर्व के इतिहास के विषय में विशेष जानकारी नहीं है; इसीलिए इस लेख के द्वारा इस महापर्व के इतिहास पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा.
पर्युषण का प्रारम्भ कब हुआ?
जैन दर्शन के अनुसार, वर्तमान अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के बहुत अल्प अन्तिम भाग में (भगवान ऋषभदेव के युग में) कुछ समय के लिए पर्युषण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई. भगवान ऋषभदेव के पश्चात् चतुर्थ आरे में भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक २२ तीर्थंकरों के युग में पर्युषण की परम्परा नहीं थी. महाविदेह क्षेत्र में भी पर्युषण इसलिए नहीं कि क्यूंकि वहाँ सर्वदा एक जैसी रहनेवाली अवस्थित कालव्यवस्था है, जो भरत क्षेत्र के चौथे आरे के समान है, अतः वहाँ पर्युषण परम्परा प्रचलित नहीं हैं[1].
जैन दर्शन के अनुसार, वर्तमान अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के बहुत अल्प अन्तिम भाग में (भगवान ऋषभदेव के युग में) कुछ समय के लिए पर्युषण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई. भगवान ऋषभदेव के पश्चात् चतुर्थ आरे में भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक २२ तीर्थंकरों के युग में पर्युषण की परम्परा नहीं थी. महाविदेह क्षेत्र में भी पर्युषण इसलिए नहीं कि क्यूंकि वहाँ सर्वदा एक जैसी रहनेवाली अवस्थित कालव्यवस्था है, जो भरत क्षेत्र के चौथे आरे के समान है, अतः वहाँ पर्युषण परम्परा प्रचलित नहीं हैं[1].
प्राचीन काल में पर्युषण की आराधना कब होती थी?
संवत्सरी का अर्थ वार्षिक पर्व है. प्राचीनकाल में पर्युषण वर्ष के अन्त में होता था; इसीलिए उसे संवत्सरी पर्व कहते हैं. श्री भगवती सूत्र में बताया गया है की जो कालमास हैं, वे श्रावण से ले कर आषाढ़ पर्यन्त बारह मास हैं - श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़. [2].
संवत्सरी का अर्थ वार्षिक पर्व है. प्राचीनकाल में पर्युषण वर्ष के अन्त में होता था; इसीलिए उसे संवत्सरी पर्व कहते हैं. श्री भगवती सूत्र में बताया गया है की जो कालमास हैं, वे श्रावण से ले कर आषाढ़ पर्यन्त बारह मास हैं - श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़. [2].
अतः प्राचीन परम्परा के अनुसार वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वर्ष पूरा होता था और श्रावण वदी १ से नूतन वर्ष प्रारम्भ होता था. जैसे कि दिन (देवसीय), रात्रि (राइय), पक्ष (पक्खी), चातुर्मासिक (चौमासी) आदि की समाप्ति पर प्रतिक्रमण किए जाते हैं, वैसे ही वर्ष भर की जीवनचर्या की आलोचना वर्ष की समाप्ति पर करनी चाहिए. इस दृष्टि से पर्युषण पर्व (संवत्सरी) की आराधना, वर्ष के अंतिम दिन, अर्थात् आषाढ़ पूर्णिमा के दिन (यानी चातुर्मास/वर्षावास स्थापना के दिन) की जाती थी.
आगम छेदसूत्र, श्री आयारदशा में श्रमणो के दस कल्पों के आठवे कल्प का नाम पज्जोसवणाकप्प (पर्युषण कल्प) है, जिसके आधार पर ही आगे चल कर श्री कल्पसूत्र की रचना हुई. इस कल्प में साधु-साध्वियों के चातुर्मास, अर्थात् वर्षावास में पालन करने योग्य आचार के विशेष नियमों का उल्लेख है. पर्युषण के दिनों में श्रमणो द्वारा पज्जोसवणाकप्प (कल्पसूत्र) के पठन की परंपरा थी, जो आज के समय में भी प्रचलित है. श्री कल्पसूत्र में साधु साध्वीजी के लिए वर्षाकाल-सम्बन्धी गमनागमन आदि विशिष्ट सामाचारी - नियमों का उल्लेख है जिसका आशय है कि वर्षा के आरंभ में ही संघ को वर्षाकालीन विधिनिषेधों का परिबोध और स्मृति हो जाए ताकि प्रसंगानुसार नियमों का शुद्ध रीति से पालन हो सके. श्री निशीथ भाष्य की चूर्णि के अनुसार पज्जोसवणाकप्प (कल्पसूत्र) चातुर्मास (वर्षावास) के आरंभ में आषाढ़ पूर्णिमा के समय ही पढ़ा जाता था, फलतः उसी समय पर्युषण होता था. [3] श्री क्षेमकीर्ति भी बृहत्कल्प भाष्य की टीका में आषाढ़ मास की समाप्ति पर कल्पसूत्र के पठन का एवं पर्युषण का उल्लेख करते है. [4]
पर्युषण की आराधना कितने दिनों के लिए होती थी?
प्राचीन ग्रन्थों विशेष रूप से श्री कल्पसूत्र एवं श्री निशीथ सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि पर्युषण मूलत: वर्षावास की स्थापना का पर्व था. श्री कल्पसूत्र के अनुसार केवल संवत्सरी का एक दिन ही पर्युषण कहलाता है. इसीलिए प्राचीन काल में ‘पर्युषण’, वर्षावास के लिए एक स्थान पर स्थिति हो जाने का एक दिन विशेष था- जिस दिन श्रमण संघ को उपवासपूर्वक केश-लोच, वार्षिक प्रतिक्रमण (सांवत्सरिक प्रतिक्रमण) और पज्जोसवणाकप्प का पाठ करना होता था. इस प्रकार पर्युषण एक दिवसीय पर्व था.
यद्यपि श्री निशीथचूर्णि के अनुसार पर्युषण के अवसर पर अट्ठम (तीन दिन का उपवास) करना आवश्यक था. श्री निशीथचूर्णि में उल्लेख है कि 'पज्जोसवणाए अट्ठम न करेइ तो चउगुरु'; अर्थात् जो साधु पर्युषण के अवसर पर अट्ठम नहीं करता है तो उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है; इसका अर्थ है कि पर्युषण की आराधना का प्रारम्भ उस दिन के पूर्व भी हो जाता था.
श्री जीवाभिगमसूत्र के अनुसार पर्युषण को अष्टाह्निक महोत्सव (आठ दिवसीय पर्व) के रूप में मनाया जाता था. उसमें उल्लेख है कि चातुर्मासिक पूर्णिमाओं एवं पर्युषण के अवसर पर देवता नन्दीश्वर द्वीप में जाकर अष्टाह्निक महोत्सव मनाया करते हैं. वर्तमान काल में आज भी आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन की पूर्णिमाओं (चातुर्मासिक पूर्णिमाओं) के पूर्व अष्टाह्निक पर्व मनाने की प्रथा है. प्राचीनकाल में पर्युषण आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता था और उसके साथ ही अष्टाह्निक महोत्सव भी होता था; हो सकता है कि बाद में जब संवत्सरी की आराधना भाद्रपद सुदी चतुर्थी/पञ्चमी को होने लगी तो उसके साथ भी आठ दिन जुड़े रहे और इसप्रकार वह अष्ट दिवसीय पर्व बन गया.
संवत्सरी की तिथि भिन्न कैसे हो गई?
सांवत्सरिक पर्व के दिन समग्र वर्ष के अपराधों और भूलों का प्रतिक्रमण करना होता है, अत: इसका समय वर्ष का अंतिम दिन ही होना चाहिये. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या पञ्चमी को किसी भी शास्त्र के अनुसार वर्ष का अन्त नहीं होता; अत: सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की वर्तमान परम्परा उत्सर्ग नहीं परन्तु अपवाद मार्ग पर आधारित है.
श्री निशीथचूर्णि में श्री जिनदासगणि ने बताया है कि पर्युषण पर्व पर वार्षिक आलोचना करनी चाहिये - “पज्जोसवनासु वरिसिया आलोयणा दायिवा”. चूँकि वर्ष की समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा को ही होती है, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को पर्युषण अर्थात् सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना चाहिए. श्री निशीथभाष्य में उल्लेख है- आषाढ़ पूर्णिमा को ही पर्युषण करना उत्सर्ग सिद्धान्त है. जिस प्रकार आज भी दिन की समाप्ति पर देवसिक, पक्ष की समाप्ति पर पक्षिक, चातुर्मास की समाप्ति पर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है, उसी प्रकार वर्ष की समाप्ति पर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाना चाहिये. पर प्रश्न होता है कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की यह तिथि भिन्न कैसे हो गई?
यह तिथि इसिलए भिन्न हुई क्यूंकि इसका एक अपवाद मार्ग बताया है. आगमों में निर्देश है की साधु (और साध्वियां) ३० दिनों से अधिक एक स्थान पर नहीं रह सकते - हालांकि चौमासे (बारिश के मौसम) के चार महीनों के दौरान, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, उन्हें एक ही जगह पर रहना चाहिए ताकि बरसात के दौरान यात्रा में होने वाली हिंसा को कम किया जा सके. प्राचीन समय में, साधुओं को आषाढ़ पूर्णिमा तक, यानी बारिश के मौसम से पहले ठहरने के लिए एक उपयुक्त निर्दोष स्थान (गुफा/उद्यान/ श्रावक के घर आदि) की आवश्यकता होती थी क्योंकि उस समय उपाश्रयों की सुविधा नहीं होती थी. उपयुक्त निर्दोष स्थान मिल जाने पर वे आषाढ़ पूर्णिमा को पर्युषण (अर्थात् संवत्सरी) की आराधना करते थे. यह था उत्सर्ग मार्ग.
अब अपवाद मार्ग के विषय में यह कहा है की यदि साधुओं को आषाढ़ पूर्णिमा तक ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं मिल रही हो तो उन्हें ५० दिन की और अनुग्रह अवधि (मुहलत) दी जाती थी. इन ५० दिनों में यदि उन्हें ठहरने का निर्दोष स्थान मिल जाता था तो वह सवंत्सरी प्रतिक्रमण और वार्षिक क्षमापना कर सकते थे (अर्थात् इन ५० दिनों में). श्री समवायांग सूत्र और श्री निशीथ सूत्र के अनुसार यदि इन ५० दिनों में भी निर्दोष जगह प्राप्त नहीं होती तो साधुओं को ५०वे दिन (यानी भाद्रपद शुक्ल ५) को एक पेड़ ने निचे सवंत्सरी प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए और इस सिमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. इससे हमें पता चलता है की भाद्रपद शुक्ल ५ सवंत्सरी प्रतिक्रमण करने का अपवादिक रूप में अंतिम दिन था.
श्री निशीथचूर्णि में स्पष्ट लिखा है कि आषाढ़ पूर्णिमा को पर्युषण करना यह उत्सर्ग मार्ग है और अन्य समय में पर्युषण करना अपवाद मार्ग है. [5] अपवाद मार्ग में भी एक मास और २० दिन अर्थात् भाद्र शुक्ल पञ्चमी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये; यदि भाद्र शुक्ल पञ्चमी तक भी निवास के योग्य स्थान उपलब्ध न हो तो वृक्ष के नीचे पर्युषण कर लेना चाहिये; अपवाद मार्ग में भी पञ्चमी, दशमी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन पर्व तिथियों में ही पर्युषण करना चाहिए, अन्य तिथियों में नहीं.
श्री कल्पसूत्र के पाठ में भी बताया गया है कि श्रमण भगवान् महावीर ने आषाढ़ पूर्णिमा से एक मास और बीस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर वर्षावास (पर्युषण) किया था उसी प्रकार गणधरों ने किया, स्थविरों ने किया और उसी प्रकार यह प्रथा प्रारम्भ हुई. [6] परन्तु श्री कल्पसूत्र में यह किस हेतु से कहा गया है, वह भी समज़ना उपयुक्त है. श्री कल्पसूत्र के पाठ का संक्षेप में भावार्थ यह है कि चूँकि इस समय तक गृहस्थ अपने मकानों को छत के रूप में आच्छादित कर लेते हैं, लीप लेते हैं, जल निकालने के लिए मोरी आदि ठीक कर लेते हैं, इत्यादि व्यवस्था हो जाने पर साधु को निर्दोष मकान मिल जाता है. ऐसे व्यवस्थित मकान में साध के निमित्त से फिर आरंभ आदि कुछ नहीं करना पड़ता, अतः वहाँ पर्युषण हो सकता है. इसका अर्थ है कि यदि प्रारंभ में ही मकान एवं क्षेत्र ठीक मिल जाए, तो आषाढ़ी पूर्णिमा आदि के दिन कभी भी पाँच-पाँच दिन के क्रम से पर्युषण कर सकता है.
इसीलिए उक्त प्रसंग में ही आगे कहा है कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद सुदी पंचमी तक बीच के पर्व दिनों में भी कभी पर्युषण कर सकते हैं, किन्तु भाद्रपद शुक्ला पंचमी की रात्रि को लांघ कर आगे नहीं कर सकते. [7]
तो फिर कुछ गच्छ भाद्रपद शुक्ल ४ को संवत्सरी की आराधना क्यों करते है?
इस बात को लेकर प्रश्न उठता है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को अपर्व तिथि में पर्युषण क्यों किया जाता है? इस सन्दर्भ में श्री निशीथ भाष्य चूर्णी और श्री कल्पसूत्र टिका में आचार्य श्री कालकसूरि की कथा दी गयी है. प्रभु महावीर के निर्वाण के ९९३ वर्ष पश्चात, यानी लगभग १०वी सदी में श्री कालिकसूरि नाम के महान आचार्य थे. वे उज्जैनी नगरी में चातुर्मास हेतु बिराजमान थे, परन्तु वहां के राजा के विरोध के कारण उन्हें वहां से विहार करके प्रतिष्ठानपुर नगरी जाना पड़ा. प्रतिष्ठानपुर पहुंच के, श्री कालिकसूरि ने वहां के राजा सत्तावाहन को भाद्रपद शुक्ल ५ के दिन सवंत्सरी प्रतिक्रमण का उपदेश दिया; तब सत्तावाहन राजा ने आचार्यश्री को बताया की उस दिन (यानी भाद्रपद शुक्ल ५ को) प्रतिष्ठानपुरमें इंद्र महोत्सव मनाया जाता है इसीलिए उन्होंने आग्रह किया की श्री कालिकसूरि भाद्रपद शुक्ल ६ (यानि एक दिन बाद) सवंत्सरी की आराधना करें.
श्री समवायांग सूत्र और श्री निशीथ सूत्र के निर्देशानुसार भाद्रपद शुक्ल ५ का उल्लंघन संभव नहीं था, इसीलिए राजा की बात रखने के लिए श्री कालकसूरिने भाद्रपद शुक्ल ४ को (यानी एक दिन पहले) राजा और सकल श्री संघ के साथ सवंत्सरी की आराधना और प्रतिक्रमण किया. यह प्रथा कायम रह गई क्योंकि शास्त्रों के अनुसार २ सवंत्सरी के बिच ३६० तिथियों जे ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए. इसी परिवर्तन की वजह से मूर्तिपूजको का बहुला वर्ग (तपागच्छ और खरतरगच्छ) आज तक भाद्रपद शुक्ल ५ की जगह भाद्रपद शुक्ल ४ के दिन सवंत्सरी की आराधना करता है. इस परिवर्तन की वजह से इन दोनों गच्छो की आराधना में निम्नलिखित बदलाव हुए -
- चातुर्मास का प्रारम्भ, आषाढ़ पूर्णिमा की जगह आषाढ़ सुदी १४ के दिन से होने लगा.
- पक्खी की आराधना जो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती थी वह भी चतुर्दशी में होने लगी.
- कार्तिक सूद १४ और फाल्गुन सूद १४ भी चातुर्मासिक आराधना (चौमासी चौदस) के रूप में निर्धारित हुए.
अमूर्तिपूजक संप्रदाय और अन्य मूर्तिपूजक गच्छो (अंचलगच्छ और पार्श्वचंद्र गच्छ) में यह परिवर्तन नहीं किए गए.
अभिवर्धित वर्ष में अधिक मास की स्थिति में पर्युषण की आराधना कैसे होती है?
पूर्व काल में कभी भी चातुर्मास के चार महिनों में किसी भी माह की वृद्धि नहीं होती थी. जैन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि बारह महिनों में से केवल पौष मास एवं आषाढ मास की ही अभिवृद्धि होती थी. तब किसी भी प्रकार की उलझन नहीं थी. पर जब से जैन पंचांगों का विच्छेद हुआ और लौकिक पंचांग को मान्यता दी गई, तब से दूसरे महीनो की भी वृद्धि होने लग गई जिसकी वजह से इस विषय में अलग अलग गच्छो/ सम्प्रदायों की अलग मान्यता हैं.
श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा के खरतरगच्छ, अंचलगच्छ और स्थानकवासी परम्परा के कुछ समुदाय (आचार्य श्री हस्तीमलजी म. का समुदाय, आचार्य श्री नानालालजी म. का समुदाय, आचार्य श्री जयमलजी म. का समुदाय, गोंडल, दरियापुरी, लिम्बडी आदि) चातुर्मास प्रारम्भ से ५० वे दिन संवत्सरी की आराधना करते हैं. इस कारण से यह गच्छ / सम्प्रदय दो श्रावण होने पर दूसरे श्रावण में तथा दो भाद्रपद होने पर प्रथम भाद्रपद में पर्युषण की आराधना करते हैं.
श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा के तपागच्छ, अमूर्तिपूजक परम्परा के स्थानकवासी (श्रमण संघ, ज्ञानगच्छ) और तेरापंथी एवं दिगंबर परंपरा के अनुसार जिस वर्ष में अधिक मास आता हो तब उस अधिक मास को कालचुला मान कर, उसे मलमास (फल्गु मास/ नपुंसक मास / पुरषोत्तम मास) मान कर उसे गिनती में नहीं लिया जाता. इस कारण से यह गच्छ / सम्प्रदय दो श्रावण होने पर भाद्रपद में पर्युषण की आराधना करते हैं.
गृहस्थों के समक्ष श्री कल्पसूत्र के वाचन की परंपरा कब प्रारंभ हुई?
प्राचीन काल में पर्युषण (संवत्सरी) के दिन साधुगण रात्रि के प्रथम प्रहर में श्री दशाश्रुतस्कन्ध (श्री आयारदशा) के आठवें अध्ययन पर्युषणकल्प का पाठ करते थे, (जो वर्तमान कल्पसूत्र का प्राचीनतम अंश है). श्री निशीथ सूत्र के अनुसार, गृहस्थों के सामने पर्युषणकल्प का वाचन निषिद्ध था. श्री निशीथ सूत्र में मुनियों को गृहस्थों एवं अन्य तैर्थिकों के साथ पर्युषण करने का चातुर्मासिक प्रायश्चित (अर्थात् १२० दिन के उपवास का दण्ड) बताया गया है. [8]
कालान्तर में इस अध्ययन (पर्युषणकल्प) के साथ श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी, श्री पार्श्वनाथ प्रभु, श्री नेमिनाथ भगवान और श्री आदिनाथ भगवान के जीवनवृत्तों एवं अन्य तीर्थंकरो के उल्लेखों तथा स्थविरावली को जोड़कर श्री दशाश्रुतस्कन्ध के आठवें अध्ययन पर्युषणकल्प को स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया जिसे आज वर्तमान में हम श्री कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं.
पर्युषण के अवसर पर गृहस्थों के समक्ष कल्पसूत्र पढ़ने की परम्परा का प्रारम्भ वीर निर्वाण के ९८० (या मतांतर से ९९३ वर्ष) के बाद आनन्दपुर नगर में ध्रुवसेन राजा (ईस्वी की पांचवी सदी में) के समय हुआ था. पर्यूषण से ठीक पहले, ध्रुवसेन राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई. तब नगर में आचार्य श्री कालिकाचार्य का चातुर्मास था; राजा शोकमग्न थे, इसीलिए प्रजा भी शोक में थी. आचार्यश्री ने सोचा की इस शोक के माहौल में पर्युषण की आराधना कैसे होगी? इसीलिए आचार्यश्री ने विचार किया और राजा को जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता का बोध कराया. शोक निवारण के लिए श्री कल्पसूत्र के वांचन का प्रारम्भ किया. तब से ले कर आज तक (यानी पिछले करीब १५०० वर्षो से) गृहस्थों के समक्ष श्री कल्पसूत्र के वाचन की परंपरा प्रारंभ हुई.
अन्य विशेष परंपराओ का प्रारम्भ
प्राचीन काल में प्रतिक्रमण, गुरुभगवंतो की उपस्थिति में किया जाता था, पर उनके साथ नहीं किया जाता था क्योंकि प्रतिक्रमण में अतिचार और अलोयणा सूत्र साधु-साध्वी और गृहस्थों (श्रावक और श्राविकाओं) के लिए भिन्न हैं. इसलिए अतीत में साधु-साध्वी और गृहस्थों के लिए अलग-अलग प्रतिक्रमण होते थे.
लगभग ५०० वर्ष पहले तपागच्छ के आचार्य श्री विजयचंद्रसूरी ने, खंभात (गुजरात) के वडी पोशाल उपाश्रय में श्रावकों के साथ प्रथम बार प्रतिक्रमण किया. प्रारंभ में अन्य आचार्यों द्वारा इसका तीव्र विरोध हुआ, परन्तु बाद में इस नई परंपरा को स्वीकार कर लिया और अब यह तपागच्छ में एक स्थायी परंपरा है.
पर्युषण में प्रभु श्री महावीर स्वामी भगवान के जन्मवांचन के पूर्व १४ स्वप्नों के चढ़ावे आदि की प्रथा प्रायः जगद्गुरु आचार्य विजय श्री हीरविजयसूरी महाराज के पश्चात् लगभग १६वी शताब्दी में प्रारम्भ हुई. प्रभु श्री महावीर के जीवन को दर्शाने वाले विशेष स्तवन (जिनको पर्युषण के प्रतिक्रमणो में बोला जाता है) की रचना भी १६ वीं शताब्दी के पश्चात् निम्नलिखित काल में हुई -
- "२७ भव के स्तवन" की रचना १९वीं शताब्दी में श्री विरविजयजी महाराज ने की,
- "हालरडा" की रचना १९वीं शताब्दी में श्री दिपजयजी महाराज ने की, और
- "पंचकल्याणक के स्तवन" की रचना १७वी शताब्दी में श्री हंसराजविजयजी ने की.
~~~~~~~
[1] जैन परम्परा में साध्वाचार सम्बन्धी दश कल्प बताए हैं- 1. आचेलक्य, 2. औद्देशिक, 3. शय्यातर पिण्ड, 4. राजपिण्ड, 5. कृतिकर्म, 6. अहिंसादि चार या पाँच महाव्रत, 7. पुरुष ज्येष्ठ धर्म, 8 प्रतिक्रमण, 9. मासकल्प ओर 10. पर्युषण कल्प. उक्त दश कल्पों में शय्यातर पिण्ड, अहिंसादि चतुर्याम व्रत, पुरुष ज्येष्ठ, कृतिकर्म- ये चार अवस्थित कल्प हैं, जो सभी 24 तीर्थंकरों के शासन में होते हैं. आचेलक्य आदि शेष छह कल्प अनवस्थित हैं. ये कल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के शासन में तो नियत होते हैं, शेष मध्यकालीन 22 तीर्थंकरों के शासन में नियत नहीं होते एवं महाविदेह क्षेत्र में भी नहीं होते.
[2] "तत्थणं जेते कालमासा तेणं सावणादीया आसाढपज्जवसाणा दुवालस पनत्ता तं जहा-सावणे भद्दवए आसोए कत्तिए मग्गसिरे से माहे फग्गुणे चेते वइसाहे जेवामूले आसाढे” - श्री भगवती सूत्र
[3] “तत्थ उ आसाढ़े पुण्णिमाए ठिया डगलादीयं गेण्हंति पज्जोसवणाकप्पं च कहेंति ।" - श्री निशीथ भाष्य चूर्णि
[4] " आषाढ़ शुद्ध दशम्यामेव वर्षाक्षेत्रे स्थितास्ततस्तेषां पंचरात्रेण डगलादौ गृहीते पर्युषणाकल्पे च कथिते आषाढ़ पूर्णिमायां 'समवसरणं' पर्युषणं भवति ।” -श्री क्षेमकीर्ति रचित बृहत्कल्प भाष्य की टीका
[5] "आसाढ़ पूणिमाए पज्जोसेवन्ति एस उसग्गो सेस कालं पज्जोसेवन्ताणं अववातो। अवताते वि सवीससतिरातमासातो परेण अतिकम्मेउण वति सवीसतिराते मासे पुण्णे जति वासखेत्तं लब्भति तो रूक्ख हेठ्ठावि पज्जोसवेयव्वं तं पुण्णिमाए पञ्चमीए, दसमीए, एवमाहि पव्वेसु पज्जुसवेयव्वं नो अपवेसु।" - श्री निशीथ चूर्णि
[6] "से केलेणं ते एवं वच्चई - समणे भगवं महावीरे वासाणं...?' ... “जओ णं पाएणं अगारीणं अगाराई कडियाई, पियाई, छन्नाई, लित्ताई, घट्टाई, मुट्टाई, संपधूमियाई, खाओदगाई, खायनिद्धमणाई, अपणो अट्ठा परिणामियाइं भवंति से तेणट्टेणं एवं वुच्चई - समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विकते वासावासं पज्जोसवेइ. ' - श्री कल्पसूत्र
[7] 'अंतरा वि य से कप्पर, नो से कप्पइतं रयणं उवाइणावित्तए.' - श्री कल्पसूत्र
[8] "जे भिक्खू अण्णउत्थिएणवा गारथिएणवा पज्जोसवेइ पज्जोसवंतं वा साइज्जइ" - श्री निशीथ सूत्र
~~~
सन्दर्भ -
· पर्युषण पर्व: एक विवेचन, डॉ. सागरमल जैन,
· पर्युषण: एक ऐतिहासिक समीक्षा, श्री अमर मुनि
· Samvatsari Pratikraman Vidhi and Explanation, Pravin K Shah
· पर्युषण पर्व महातम्य, स्मिता पि. शाह
· पर्युषण अने तेनो उपयोग, पंडित सुखलाल संघवी
सन्दर्भ -
· पर्युषण पर्व: एक विवेचन, डॉ. सागरमल जैन,
· पर्युषण: एक ऐतिहासिक समीक्षा, श्री अमर मुनि
· Samvatsari Pratikraman Vidhi and Explanation, Pravin K Shah
· पर्युषण पर्व महातम्य, स्मिता पि. शाह
· पर्युषण अने तेनो उपयोग, पंडित सुखलाल संघवी

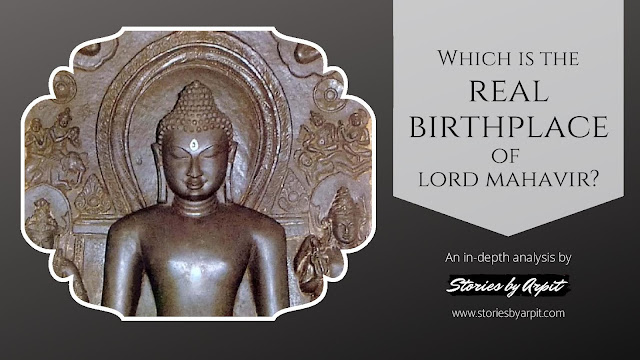








Nice and almost factual presentation of Paryushana. Kudos, Arpitbhai 👌
ReplyDeleteThanks for such elaborate article! 🙏
ReplyDelete