क्या हम वास्तव में जैन है? ...या कुछ और ?
बहुत वर्षों पहले की बात है.
मैं और कुछ मित्र तीर्थ यात्रा पे निकले थे और वहां पहुंचते पहुंचते देर रात हो गई थी. कमरे के लिए पूछते ही धर्मशाला के मैनेजर ने कार्यवाही शुरू की-
“कौन है - कहाँ से आये हैं - कितने दिन रुकेंगे - आप जैन है या नहीं” आदि.
वहाँ तक सब ठीक था.
फिर अचानक सवाल आया – “आप कौनसे पंथी हो?”
मेरे कान खड़े हो गए - ये कैसा सवाल था?
मैंने पूछा - “कौनसे पंथी मतलब?”
तब उन्होंने थोडे विस्तार से पूछा – “कौन से पंथ के हो - श्वेतांबर या दिगंबर?”
मैंने कहा – ‘श्वेतांबर’ - और साथ-साथ मैने भी एक सवाल जड़ दिया –“क्यों ऐसा पूछ रहे हो ?”
तो उन्होंने जवाब दिया – “फॉर्म में सब लिखना पड़ता है. सभी पंथ के लोग उतरते है यहाँ.”
मैंने सोचा, चलो ठीक है.
मुझे लगा के पूछताछ ख़त्म हो गई तभी सामने से और एक सवाल आया - "मंदिर-मार्गी (मूर्तिपूजक) हो ना?"
मैंने जवाब दिया - 'हां'. तुरंत एक और सवाल आया – “तपागच्छ के हो या खरतरगच्छ के?”
मैने गुस्से में कह दिया - "आपको मतलब? क्या यह भी फॉर्म में लिखना है?"
तो उन्होंने हस्ते हस्ते कहा - "नहीं-नहीं, मुझे तो बस जानना था के आप नौजवानो को पता भी है या नहीं".
मेरा मित्र जो इतनी देर से पीछे चुपचाप खड़ा था उसने उत्साहित होकर जवाब दिया – “जी हां ! हमें पता है हम तपागच्छ के 'फलाने' समुदाय से हैं !”
मै भौचक्का रह गया ! मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा मित्र भी इस समुदायवाद में फसा हुआ है !
कार्यालय से निकलते वक्त मैनेजर ने मेरे मित्र को धीरे से कहा - "अच्छा है आप 'फलाने' समुदाय के नहीं है - वह लोग तो पुरे मिथ्यात्वी है !"
मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था.
उस रात, बेचैनी में, मुझे नींद नहीं आयी.
~~~~~~~~~~~~~~
जैन धर्म में प्राचीन काल से दिगंबर और श्वेतांबर ये दो मूल शाखाएँ तो है ही, किन्तु वे शाखाएँ भी सम्प्रदायों में विभाजित हो चुकी है. दिगंबर परंपरा में बीसपंथ, तेरापंथ, तारणपंथ, गुमानपंथ एवं तोतापंथ उपसम्प्रदाय के साथ-साथ कानजी स्वामी के अनुयायियों का भी नया संप्रदाय बन गया है. श्वेतांबर परंपरा भी मूर्तिपूजक, स्थानकवासी एवं तेरापंथ में विभाजित हो चुकी है. इनके अतिरिक्त भी "यापनीय" नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय दूसरी शताब्दी से ले कर १५वी शताब्दी तक अस्तित्व में रहा जो आज विलुप्त हो गया है. आश्चर्य की बात यह है की यह संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर परम्पराओ की मध्यवर्ती कड़ी के रूप में था -यह संप्रदाय तीर्थंकरो (एवं साधुओं) की नग्नता को स्वीकार करता था (अपितु अपवाद वश एक वस्त्र भी धारण करता था) परन्तु साथ-साथ श्वेतांबर आगमो को मानता था और स्त्री मुक्ति को भी स्वीकार करता था (जिन दोनों का निषेध दिगंबर करते हैं). वर्तमान में श्रीमद राजचन्द्र एवं दादा भगवान भी एक तरह से स्वतंत्र संप्रदाय बन चुके है.
ऊपर दी गई तस्वीर से हम समझ सकते हैं की हम कितने सम्प्रदायों में बटें हुए है. परन्तु यह विभाजन यहाँ समाप्त नहीं होते - ये शाखाऐं भी गच्छो और समुदायों में विभाजित हो चुकी है. उदहारण के तौर पे निचे दी हुई तस्वीर से हम देख सकते हैं की श्वेतांबर मूर्तिपूजक संप्रदाय भी कितने गच्छो और समुदायों में बंट चूका है. (यहाँ गौर करने जैसा है की मात्र मूर्तिपूजक ही नहीं, लगभग अन्य सारे सम्प्रदाय भी, गच्छ, संघ और समुदायोंमे विभाजित हो चुके है)
मै भौचक्का रह गया ! मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा मित्र भी इस समुदायवाद में फसा हुआ है !
कार्यालय से निकलते वक्त मैनेजर ने मेरे मित्र को धीरे से कहा - "अच्छा है आप 'फलाने' समुदाय के नहीं है - वह लोग तो पुरे मिथ्यात्वी है !"
मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था.
उस रात, बेचैनी में, मुझे नींद नहीं आयी.
~~~~~~~~~~~~~~
जैन धर्म में प्राचीन काल से दिगंबर और श्वेतांबर ये दो मूल शाखाएँ तो है ही, किन्तु वे शाखाएँ भी सम्प्रदायों में विभाजित हो चुकी है. दिगंबर परंपरा में बीसपंथ, तेरापंथ, तारणपंथ, गुमानपंथ एवं तोतापंथ उपसम्प्रदाय के साथ-साथ कानजी स्वामी के अनुयायियों का भी नया संप्रदाय बन गया है. श्वेतांबर परंपरा भी मूर्तिपूजक, स्थानकवासी एवं तेरापंथ में विभाजित हो चुकी है. इनके अतिरिक्त भी "यापनीय" नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय दूसरी शताब्दी से ले कर १५वी शताब्दी तक अस्तित्व में रहा जो आज विलुप्त हो गया है. आश्चर्य की बात यह है की यह संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर परम्पराओ की मध्यवर्ती कड़ी के रूप में था -यह संप्रदाय तीर्थंकरो (एवं साधुओं) की नग्नता को स्वीकार करता था (अपितु अपवाद वश एक वस्त्र भी धारण करता था) परन्तु साथ-साथ श्वेतांबर आगमो को मानता था और स्त्री मुक्ति को भी स्वीकार करता था (जिन दोनों का निषेध दिगंबर करते हैं). वर्तमान में श्रीमद राजचन्द्र एवं दादा भगवान भी एक तरह से स्वतंत्र संप्रदाय बन चुके है.
ऊपर दी गई तस्वीर से हम समझ सकते हैं की हम कितने सम्प्रदायों में बटें हुए है. परन्तु यह विभाजन यहाँ समाप्त नहीं होते - ये शाखाऐं भी गच्छो और समुदायों में विभाजित हो चुकी है. उदहारण के तौर पे निचे दी हुई तस्वीर से हम देख सकते हैं की श्वेतांबर मूर्तिपूजक संप्रदाय भी कितने गच्छो और समुदायों में बंट चूका है. (यहाँ गौर करने जैसा है की मात्र मूर्तिपूजक ही नहीं, लगभग अन्य सारे सम्प्रदाय भी, गच्छ, संघ और समुदायोंमे विभाजित हो चुके है)
 |
लगभग ८०० करोड़ की जनसँख्या वाली इस पृथ्वी पर जैनो की संख्या मात्र ४५ लाख है - इस समग्र विश्व की मात्र ०.०६ फीसदी जनता जैन है. दुर्भाग्य यह है की एक अल्पसंख्यक धर्म होते हुए भी आज हम अनेक पंथ -संप्रदाय एवं उपसम्प्रदाय में बंट चुके है. पर मुझे इस बात का दुःख नहीं है की हम इतने पंथो में बटें हुए है - यह बात तो स्वयं प्रभु महावीरने फ़रमाई थी. मुझे दुःख इस बात का है की यह सारे पंथ परस्पर एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते है- एक दूसरे को मिथ्यात्वी बताते है, अपने मत को दूसरे से श्रेष्ठ बतातें हैं. तकलीफ इस बात की है की अंतरमें हम सब पहले दिगंबर-श्वेतांबर-स्थानकवासी-तेरापंथी है, बाद में जैन है. इस बात को हम प्रत्यक्ष देख सकते है - दिगंबर संप्रदाय की हर संस्था में पहले "दिगंबर" शब्द आता है और फिर "जैन" शब्द जोड़ा जाता है (मात्र उदहारण के तौर पे - श्री दिगंबर जैन महासभा). श्वेतांबर संघ बस नाम में पहले जैन शब्द को जोड़ता है - बाकि वह भी अपने मत को दूसरों से श्रेष्ठ बताता है.
आज का जैन समाज पारस्परिक संघर्षो, विवादों और आडम्बरो की प्रतिस्पर्धा में लग चूका है. श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, श्री केशरियाजी, श्री मक्षीजी, श्री शिखरजी जैसे तीर्थो का विवाद आज भी चालू है. जिस प्रभुकी प्रतिमाजी को हम साक्षात् तीर्थंकर मानते हैं उसके साथ हम क्या-क्या कुकर्म नहीं कर रहे? कभी उबलता दूध डालके लेप को निकाला जाता है, गरम शलाखो से चक्षुओं को रोज निकाला और लगाया जाता है और कटिसूत्र-कन्डोरे को लोहे के औज़ार द्वारा तोडा जाता है ! क्या यह सब हमारी अंतरआत्मा को कचोटता नहीं है? पारस्परिक संघर्षो में उन तीर्थोंमें घटनाए घटित हुई है वे क्या एक अहिंसक समाज के लिए शर्मनाक नहीं है? पत्र-पत्रिकाओंमें एक दूसरे के विरुद्ध जो विष-वमन किया जाता है, क्या हमारे हृदयको विक्षोभित नहीं करता है? बात इस हद तक बढ़ चुकी है की बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है की (अपने ही धर्म के) दूसरे संप्रदाय के मंदिरो में जाने से पाप लगता है और वहां बिराजमान (अपने ही परमात्मा की) प्रतिमाका दर्शन करने से मिथ्यात्व का दोष लगता है; और आजकल तो ऐसा भी सिखाया जाता है दूसरे संप्रदाय या दूसरे समुदाय के गुरुओं को वंदन करने से और उनको गोचरी वोहराने से दोष लगता है. आश्चर्य की बात तब होती है जब लोग इसका शब्द दर शब्द पालन करते है !
 |
इन सारी बातो की और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक गुरुभगवंतो एवं पंडितो से मुलाकात की; लगभग सभी से बात करके मुझे सांप्रदायिक पूर्वाग्रहो का आभास हुआ. सभी अपने आप और अपने मत को सही बता रहे थे और दुसरो के मत को मित्थ्यात्व बता रहे थे. मै और असमंजस में पड़ गया. अनेक मित्रों ने सलाह भी दी - "यह सब चक्कर में मत पड़ो - अपने गुरुदेव जो कहते हैं, वही सत्य है. औरों की बातो पर मत ध्यान दो." अपने मत के प्रति ऐसी पूर्वाग्रही देख के मेरा मन काफी व्यथित हुआ. तभी मेरे अध्ययन की एक पुस्तक में महापवित्र श्री उत्तराध्ययन सूत्र की कुछ पंक्तियां सामने आयी –
हमारे पंथवाद के कारण -
१. गुणपूजा से व्यक्तिपूजा - जो जैन गुणपूजक था, वह आज व्यक्ति (गुरु) उपासना में जुड़ गया है. यह बात ज़रूर है की पूज्य गुरुदेवो के उपकारों से ही हम प्रभु के मार्ग तक पहुंच सके है, पर उसका यह अर्थ तो नहीं है की हम उनके गुणों की पूजा छोड़ उनके व्यक्तित्व की पूजा करने लग जाएं. आजकल तो, १४ पूर्वधर श्री भद्रबाहु स्वामी और कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य से ज़्यादा वर्तमान धर्माचार्यों की स्तुति और स्तवना होती है! नमस्कार महामंत्र के तीसरे,चौथे और पांचवे पद का स्मरण करते वख्त हमें विश्व के समस्त आचार्यों के ३६ गुण, उपाध्यायों के २५ गुण, और साधुओँ के २७ गुणों को नमस्कार करना है - न की अपने ही संप्रदाय या समुदाय के गुरुओं की व्यक्तिगत वंदना करनी है. इस व्यक्तिपूजा की वजह से इंसान को अपने धर्माचार्य के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है और इसी रागात्मकता के कारण वह अपने गुरु के संप्रदाय और उनके मत को अंतिम सत्य मान लेता है. इसके परिणामस्वरूप दूसरों के मत के प्रति द्वेषभाव उत्पन्न हो जाता है. हो सकता है की अपने धर्माचार्य और उनका मत ही सत्य है - पर इससे हमें दूसरे मतों को मिथ्यात्वी कहने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता. मै यह भी नहीं कहता के हम दूसरे संप्रदायों के मतों को सत्य स्वीकार लें - पर कमसेकम उन मतों के प्रति द्वेष भाव रखना और उन्हें मिथ्यात्व कहना तद्दन अनुचित है. महापवित्र आगम ग्रन्थ श्री सूत्रकृतांग सूत्र में प्रभु श्री महावीरने फ़रमाया है की -
“सयं सयं पसंसंता गरहंता परं वयं।
जे उ तत्थ विउस्संति संसारे ते विउस्सिया ।।"
जो लोग अपने-अपने मत की प्रशंसा और दूसरे मत की निंदा करते है तथा दुसरो के प्रति द्वेष का भाव रखते है वे संसार में परिभ्रमण करते रहते है.
२. अनेकांतवाद के सिद्धांत को भुला देना – आज दुर्भाग्य की बात यह है, की जो धर्म, प्रभु श्री महावीर द्वारा बताये हुए अनेकांतवाद के सिद्धांत के द्वारा विभिन्न दर्शनों में समन्वय की बात करता है और जो "षट्दरसण जिन अंग भणीजे" की व्यापक द्रष्ट्रि प्रस्तुत करता है वह स्वयं अपने ही सम्प्रदायों के बिच समन्वय सूत्र नहीं खोज पा रहा है. एक ओर अनेकांतवाद का उद्घोष और दूसरी ओर सम्प्रदायों के बिच में द्वेष भाव - दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते. आज यह सिद्धांत मात्र पुस्तकों में पढ़ा जा सकता है - उसका आचरण जैसे हम सबने भुला दिया है.
- “अप्पणा सच्चमेसेज्जा” – “अपने द्वारा और अपने चिंतन मनन के द्वारा सत्य की खोज करनी चाहिए”
- “पन्ना समिक्खए धम्मं”- “प्रज्ञा चक्षु से धर्म की समीक्षा करनी चाहिए (ना की जड़ हो कर).
हमारे पंथवाद के कारण -
१. गुणपूजा से व्यक्तिपूजा - जो जैन गुणपूजक था, वह आज व्यक्ति (गुरु) उपासना में जुड़ गया है. यह बात ज़रूर है की पूज्य गुरुदेवो के उपकारों से ही हम प्रभु के मार्ग तक पहुंच सके है, पर उसका यह अर्थ तो नहीं है की हम उनके गुणों की पूजा छोड़ उनके व्यक्तित्व की पूजा करने लग जाएं. आजकल तो, १४ पूर्वधर श्री भद्रबाहु स्वामी और कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य से ज़्यादा वर्तमान धर्माचार्यों की स्तुति और स्तवना होती है! नमस्कार महामंत्र के तीसरे,चौथे और पांचवे पद का स्मरण करते वख्त हमें विश्व के समस्त आचार्यों के ३६ गुण, उपाध्यायों के २५ गुण, और साधुओँ के २७ गुणों को नमस्कार करना है - न की अपने ही संप्रदाय या समुदाय के गुरुओं की व्यक्तिगत वंदना करनी है. इस व्यक्तिपूजा की वजह से इंसान को अपने धर्माचार्य के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है और इसी रागात्मकता के कारण वह अपने गुरु के संप्रदाय और उनके मत को अंतिम सत्य मान लेता है. इसके परिणामस्वरूप दूसरों के मत के प्रति द्वेषभाव उत्पन्न हो जाता है. हो सकता है की अपने धर्माचार्य और उनका मत ही सत्य है - पर इससे हमें दूसरे मतों को मिथ्यात्वी कहने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता. मै यह भी नहीं कहता के हम दूसरे संप्रदायों के मतों को सत्य स्वीकार लें - पर कमसेकम उन मतों के प्रति द्वेष भाव रखना और उन्हें मिथ्यात्व कहना तद्दन अनुचित है. महापवित्र आगम ग्रन्थ श्री सूत्रकृतांग सूत्र में प्रभु श्री महावीरने फ़रमाया है की -
“सयं सयं पसंसंता गरहंता परं वयं।
जे उ तत्थ विउस्संति संसारे ते विउस्सिया ।।"
जो लोग अपने-अपने मत की प्रशंसा और दूसरे मत की निंदा करते है तथा दुसरो के प्रति द्वेष का भाव रखते है वे संसार में परिभ्रमण करते रहते है.
२. अनेकांतवाद के सिद्धांत को भुला देना – आज दुर्भाग्य की बात यह है, की जो धर्म, प्रभु श्री महावीर द्वारा बताये हुए अनेकांतवाद के सिद्धांत के द्वारा विभिन्न दर्शनों में समन्वय की बात करता है और जो "षट्दरसण जिन अंग भणीजे" की व्यापक द्रष्ट्रि प्रस्तुत करता है वह स्वयं अपने ही सम्प्रदायों के बिच समन्वय सूत्र नहीं खोज पा रहा है. एक ओर अनेकांतवाद का उद्घोष और दूसरी ओर सम्प्रदायों के बिच में द्वेष भाव - दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते. आज यह सिद्धांत मात्र पुस्तकों में पढ़ा जा सकता है - उसका आचरण जैसे हम सबने भुला दिया है.
कुछ विवादों पर विचार -
A. तीर्थंकरो के स्वरूप का विवाद - श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विवाद का मूल कारण नग्नत्व का ही है. जहां दिगंबर ग्रन्थ यह उद्घोष करते हैं की सभी तीर्थंकर अचेल (नग्न) होकर दीक्षित होते हैं वहां श्वेतांबर ग्रन्थ यह कहते हैं की सभी तीर्थंकर एक देवदूष्य वस्त्र ले कर दीक्षित होते है. प्राचीनतम आगम श्री आचारांग सूत्र में बताया गया है की प्रभु श्री महावीर ने भी देवदूष्य धारण करके दीक्षा ग्रहण की थी, परन्तु उन्हें उस वस्त्र के प्रति कोई आसक्ति या परिग्रह नहीं था -मात्र इंद्र की विनंती को स्वीकृती रूप उन्होंने देवदूष्य को धारण किया था. दीक्षा के १३ महीने बाद उन्होंने उसे भी त्याग दिया था और उसके बाद निर्वाण तक प्रभु अचेल रहें. इसी देवदुष्य - नग्नता के अंतर की वजह से दिगंबर संप्रदाय तीर्थंकरों की नग्न प्रतिमा की पूजा करता है और श्वेताम्बर संप्रदाय अपनी प्रतिमाओं में कटिवस्त्र-कंडोरे (वस्त्र चिह्न) का अंकन करता है.
उपाध्याय श्री मेघविजयजी ने 'युक्तिप्रबोध' नामक ग्रन्थ में फ़रमाया है की तीर्थंकर प्रभु की निर्वस्त्र प्रतिमा देख के शायद दर्शन करने वाले के मन (खास कर के स्त्रियों के मन में) में गलत ख्याल आ सकते है. उन्होंने यह भी फ़रमाया है की अतिशयों के प्रभाव से तीर्थंकरों के शरीर का इतना तेज होता है की वह चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता - इसीलिए प्रभु का नग्न स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता - और इसी वजह से उनके निर्वस्त्र स्वरूप की प्रतिमा बनाना अनुचित है. परन्तु इसी विषय को यदि हम मूर्तिमंडन और पुरातात्विक दृष्टी से देखें तो हमें पता चलता है की लगभग ईस्वी की पांचवी सदी तक (प्रभु श्री महावीर के निर्वाण के पश्चात लगभग १००० वर्ष पश्चात) श्वेतांबर और दिगंबर प्रतिमाओं में भेद नहीं होता था. दोनों संप्रदाय एक ही जिनबिम्ब की पूजा अर्चना करते थे. इस बात का प्रमाण मैं निम्नलिखित बातों से देने का प्रयास करता हूँ -
१. मथुरा के कंकाली टीले स्थित जैन स्तूप से जो ईस्वी पूर्व प्रथम सदी से ले कर ईसा की प्रथम द्वित्य सदी तक की प्राचीन जिन प्रतिमाऐं प्राप्त हुई है वह सभी निर्वस्त्र है (पद्मासन मुद्रा की जिन प्रतिमाओं में न तो नग्नत्व का प्रदर्शन होता था और न वस्त्र का चिह्न बनाया जाता था; जो कार्योत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमाजी थी उनमे स्पष्ट रूप से नग्न स्वरूप दर्शाया जाता था). किन्तु इन प्रतिमाओं के निचे जो अभिलेख उपलब्ध है और उनमे जिन आचार्यों के कुल, शाखा एवं गण आदि के उल्लेख हैं, वह श्वेतांबर हैं. उनके नाम श्वेतांबर मान्य श्री कल्पसूत्र की स्थविरावली में भी प्राप्त होते हैं. इस बात से स्पष्ट पता चलता है की पूर्व काल में श्वेतांबर संघ निर्वस्त्र प्रतिमाओं की आराधना करता था और उनके धर्माचार्यों द्वारा इन निर्वस्त्र प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी हुई थी.
१. मथुरा के कंकाली टीले स्थित जैन स्तूप से जो ईस्वी पूर्व प्रथम सदी से ले कर ईसा की प्रथम द्वित्य सदी तक की प्राचीन जिन प्रतिमाऐं प्राप्त हुई है वह सभी निर्वस्त्र है (पद्मासन मुद्रा की जिन प्रतिमाओं में न तो नग्नत्व का प्रदर्शन होता था और न वस्त्र का चिह्न बनाया जाता था; जो कार्योत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमाजी थी उनमे स्पष्ट रूप से नग्न स्वरूप दर्शाया जाता था). किन्तु इन प्रतिमाओं के निचे जो अभिलेख उपलब्ध है और उनमे जिन आचार्यों के कुल, शाखा एवं गण आदि के उल्लेख हैं, वह श्वेतांबर हैं. उनके नाम श्वेतांबर मान्य श्री कल्पसूत्र की स्थविरावली में भी प्राप्त होते हैं. इस बात से स्पष्ट पता चलता है की पूर्व काल में श्वेतांबर संघ निर्वस्त्र प्रतिमाओं की आराधना करता था और उनके धर्माचार्यों द्वारा इन निर्वस्त्र प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी हुई थी.
२. दिगंबरों और श्वेतांबरों के बिच गिरनार पर्वत के स्वामित्व को ले कर जो निम्नलिखित विवाद उठे है उससे हम समज सकते हैं की दोनों संप्रदाय एक ही जिनबिम्ब की आराधना करते थे -
- श्री उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थमें श्री रत्नमंदिरगणिवर्य ने लिखा है की आचार्य बप्पभटसूरीश्वरजी महाराजा के समयमे गिरनार तीर्थ दिगंबरो के स्वामित्वमें था (इससे यह अनुमान लगा सकते है की प्रतिमाजी पे कटिसूत्र-कन्डोरा नहीं था). आचार्यश्रीने दिगंबरों से वाद किया और अंतमें अम्बिका देवीने "उज्जिंत सेल सिहरे" गाथा कह कर विवादकी समाप्ति कर दी (गाथामें यह कहा गया है की चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, प्रभुकी वाणी सभी को मुक्ति तक पहुंचाने में समर्थ है). दिगंबर, स्त्री मुक्तिमे नहीं मानते इसीलिए अम्बिका देवी के कथानुसार वाद में श्वेतांबर संप्रदाय के पक्ष में हुआ.
- श्री सुखसागर ग्रन्थमें श्री रत्नमण्डनगणिवर्य ने लिखा है की १३वी सदीमे श्वेतांबर सम्प्रदाय के श्री पेथडशाह मंत्री और दिगंबर संप्रदाय श्री पूर्णचंद्र अग्रवाल गिरनार पर्वत पे संघ ले कर आये. गिरनार की तलहटी पे पूर्णचंद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय के यात्रिओं को चढ़ने से रोका और दोनों संप्रदाय के लोगो के बिचमें तीर्थके स्वामित्व को ले कर विवाद उत्पन्न हुआ. बुजुर्गो ने रास्ता निकाला की जो इन्द्रमाल (संघमाल) की बोली जीतेगा, वह तीर्थ उसका होगा. सभी ने सहमति दी और दोनों सम्प्रदय के यात्रिओं ने साथ में पर्वत का आरोहण किआ. मूल मन्दिरमे दोनों संप्रदाय के यात्रिओं ने मूलनायक प्रतिमाजी के समक्ष पूजा-अर्चना, नृत्य-स्तुति गान एवं ध्वजारोपण किआ. (इस बात से सिद्ध होता है की १३वी सदी तक दोनों संप्रदाय की प्रतिमाओं एवं पूजा विधि में भिन्नता नहीं थी) . इन्द्रमाल के समय पे पेथडशाह मंत्रीने ५६ घडी सोना (लगभग १२०० किलो) की बोली लगा के जिनालय एवं मूलनायक प्रतिमा को श्वेतांबर संघ के अधीन किया.
- श्री प्रवचनपरीक्षा ग्रन्थमें उपाध्याय श्री धर्मसागरजीने लिखा है की दिगंबरों और श्वेतांबरों के बिच गिरनार पर्वत के स्वामित्व को ले कर जो विवाद उठा उसके बाद ही श्वेतांबर परंपरा की प्रतिमाओं में वस्त्र चिह्न बनाने की प्रथा शुरू हुई.
३. हलसी गाँव (कर्नाटक) से प्राप्त हुए राजा मृगेशवर्मन के १६०० वर्ष प्राचीन ताम्र अभिलेखों से पता चलता है की दिगंबर, यापनीय और श्वेतांबर संघ के मंदिर और प्रतिमाएँ भिन्न नहीं थी - सभी एक ही जिनमंदिर में आराधना करते थे.
४. श्री उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थमें श्री रत्नमंदिरगणिवर्य ने लिखा है की १२वी सदीमे वस्तुपाल-तेजपाल मंत्रीने एक संघ निकाला था जिसमे २४ हाथी दांत के देवालय थे, १२० काष्ठ के देवालय थे, ४५०० (घोड़े) गाड़िया, १८०० डोलियां, ५०० पालखी, ७०० आचार्य, २००० श्वेतांबर साधु और ११०० दिगंबर साधु आदि अनेक श्वेतांबर - दिगंबर श्रावक-श्राविका थे. इससे यह मालूम होता है की उस समय तक तीर्थ यात्रा, पूजन विधि आदि में दिगंबर एवं श्वेतांबरोमे इतनी भिन्नता नहीं थी. दोनोमे वैर भाव भी नहीं था और उनकी प्रतिमाओं में भी अंतर नहीं था क्योंकि अगर अंतर होता तो ग्रंथमे दिगंबरोके देवालयों की भी संख्या दी होती.
५. अकबर प्रतिबोधक जगद्गुरु आचार्यश्री हिरविजयसूरीश्वरजी महाराजाने १६वी सदीमे मथुरा से लौटते हुए गोपाचल (ग्वालियर) स्थित बावनगजा श्री आदिनाथ भगवान की दिगंबर प्रतिमा के दर्शन किये थे (जो आज भी मौजूद है). इससे साबित होता है की श्वेतांबर सम्प्रदायके आचार्य भी नग्न प्रतिमा के दर्शन करते थे.
६. तपागच्छ के मुनि श्री शीलविजयने १७वी सदीमे दक्षिण के मूडबिद्री, कारकल, हुमचा आदि अनेक दिगंबर तीर्थो की यात्रा की थी और भक्तिभाव से उनकी वंदना भी की थी. बड़े उत्साह से उन दिगंबर तीर्थो और प्रतिमाओं की प्रशंसा की थी. यह सब उन्होंने अपनी तीर्थमाला में लिखा है. इससे मालूम होता है की उस समय भी श्वेतांबर साधु, तीर्थंकरो की नग्न प्रतिमाको समान आदर से दर्शन करते थे.
 |
इन सब बातों से जब यह सिद्ध होता है की पूर्व काल में श्वेतांबर और दिगंबर प्रतिमाएं एक ही स्वरुपमे पूजी जाती थी और श्वेतांबर जैन संत दिगंबर प्रतिमाओं को नमन करते थे तो फिर आज क्यों परस्पर हम एक दूसरे को मिथ्यात्वी कहते हैं? क्यों एक दूसरे के मंदिरों में जाने पे रोक लगातें हैं? जब-जब भी मैं यह सवाल “चुस्त आराधकों” पूछता हूँ तब- तब मुझे वही पुराना जवाब मिलता है – “दूसरे पंथो के मंदिरो में जाने से - (१) मिथ्यात्व का दोष लगता है (क्योंकि वहां बिराजमान भगवान मान्य स्वरूप में नहीं है) (२) सम्यक्त्व मलिन होता है और हम सम्यक्त्व गवां भी सकते है , (३) दूसरे पंथ का आकर्षण लग सकता है क्योंकि 'हम श्रावकों' को शास्त्रों की सही समझ नहीं है और हम नादान बालक की तरह हैं ! (४) हमें देख के और भी श्रावक दूसरे पंथ में जाना शुरू कर सकते हैं !”
किस हद्द तक यह सांप्रदायिक डर हमारे अंदर घुस गया है उसका यह प्रत्यक्ष उदहारण है - और यही बात बचपन से सिखाई जाती है जिससे इंसान के अवचेतन मन में यह बात सम्पूर्ण रूप से जम जाती है. अभी कुछ महीनों पहले ही मैंने इसका स्वयं अनुभव किया था - तीर्थ यात्रा के दौरान एक प्राचीन तीर्थ में जाना हुआ जहाँ लगभग १६०० वर्ष प्राचीन जिन प्रतिमा बिराजमान है. इतिहास गवाह है की प्राचीन काल में दोनों श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के आराधक इस मंदिर को अपनी श्रद्धा का केंद्र स्थान मानते थे, परन्तु पिछले सौ वर्षों से वह तीर्थ दिगंबर संप्रदाय के प्रबंधन में था. वहां बिराजमान मूलनायक प्रभु की अद्भुत और दिव्य प्रतिमाजी के दर्शन कर के मेरा मन झूम उठा, पर मेरे साथ आये एक मित्र ने प्रभु के सामने अपना माथा भी नहीं झुकाया ! और आश्चर्य की बात तो यह थी की प्रभु की प्रतिमा भी पद्मासन मुद्रा में थी -नग्नता का कोई चिह्न भी नहीं था - फिर भी मेरे मित्र को उस प्रतिमा में प्रभु नहीं दिख रहे थे !
उपाध्याय श्री मेघविजयजी के युक्तिप्रबोध ग्रन्थ से मैं भी सहमत हूँ - पर इससे मुझे इस बात का अधिकार नहीं मिल जाता की मैं दूसरे स्वरूपों को मिथ्यात्व मान लूँ. मैं आशा रखता हूँ की इस लेख को पढ़ने वाला प्रबुद्ध वर्ग यह सब तथ्य समझने के बाद श्री तीर्थंकर प्रभु के किसी भी स्वरूप में, चाहे वह अंगरचना से सजा हुआ रूप हो या ध्यानमग्न वीतरागी स्वरूप हो- सभी में अरिहंत परमात्मा के दर्शन कर पाए.
~~~~~~~~~~~~~~
B. मुनिओं के वस्त्र सम्बन्धी आचारो का विवाद: अगर मुनिओं के वस्त्र सम्बन्धी आचारों की बात करें तो आगम ग्रन्थ श्री उत्तराध्ययन सूत्र से हमें पता चलता है की प्रभु पार्श्वनाथ के साधुओं की परंपरा सचेल (वस्त्रधारी) रही थी. साथ-साथ श्री आचारांग सूत्र और बौद्ध त्रिपिटको (ग्रंथो) से हमें पता चलता है की प्रभु महावीर स्वामी के संघमें सचेल (वस्त्रधारी) और अचेल (निर्वस्त्र) दोनों प्रकार के श्रमणो का समावेश था. जिनकल्पी साधु (अर्थात् 'जिन'- तीर्थंकर के सामान आचरण करने वाले मुनि) नग्न रहते थे यह बात की स्वीकृति श्वेतांबर आगम देते हैं (यह अवस्था हर तीर्थंकर के काल में थी)- परन्तु समय के प्रवाह में इस अवस्था का विच्छेद हुआ.
दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है की मात्र अचेल (नग्न) ही मुनि पद का अधिकारी है; हालांकि दिगंबर ग्रन्थ श्री भगवती आराधना की टिका में भी अपवादिक स्थितिओ में एक मुनि को वस्त्र ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. एलक और क्षुल्लक के रूप में आज भी दिगंबर परंपरा ऐसे मुनिओं को स्वीकार करती है जो अल्प वस्त्रों को धारण करते हैं. यापनीय परंपरा का दृश्टिकोण इन दोनों पक्षों के मध्य का समन्वय करता है - यह परंपरा की मान्यता है की सामान्यतः मुनि को अचेल (नग्न) रहना चाहिए क्योंकि वस्त्र भी परिग्रह है, किन्तु अपवादिक स्थितिओं में संयमोपकरण के रूप में वस्त्र रखा जा सकता है.
प्राचीनतम आगम श्री आचारांग सूत्र में वस्त्र सम्बन्धी चार प्रकार के मुनिओं का उल्लेख है –
१. अचेल - जो मुनि हमेंशा नग्न रहते थे - अर्थात् जिनकल्पी
२. एक वस्त्र धारी - लोक लज्जा निवारण और सर्दियों में शीत निवारण के जो मुनि अपने पास एक वस्त्र रखते थे. कुछ मुनि मात्र एक लंगोट पहनते थे
३. दो वस्त्र धारी - जो मुनि एक अधोवस्त्र और एक उत्तरीय वस्त्र रखते थे
४. तीन वस्त्र धारी - जो मुनि अधोवस्त्र और उत्तरीय के साथ एक कम्बल रखते थे.
श्री आचारांग सूत्रमें में यह भी कहा गया है की –
१. जो मुनि युवान, बलवान, निरोगी हो उसे एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए
२. जो मुनि लज्जा को जित सकता है उसे अचेल रहना चाहिए और तृणस्पर्श ,ठण्ड, ताप मच्छर आदि के उपद्रवों को और परिषह को सहन करना चाहिए.
३. जो मुनि लज्जा आदि परिषह को सहन नहीं कर सकता, वह कटिबंध वस्त्र (चोलपट्टा) रख सकता है.
३. दो वस्त्र धारी - जो मुनि एक अधोवस्त्र और एक उत्तरीय वस्त्र रखते थे
४. तीन वस्त्र धारी - जो मुनि अधोवस्त्र और उत्तरीय के साथ एक कम्बल रखते थे.
श्री आचारांग सूत्रमें में यह भी कहा गया है की –
१. जो मुनि युवान, बलवान, निरोगी हो उसे एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए
२. जो मुनि लज्जा को जित सकता है उसे अचेल रहना चाहिए और तृणस्पर्श ,ठण्ड, ताप मच्छर आदि के उपद्रवों को और परिषह को सहन करना चाहिए.
३. जो मुनि लज्जा आदि परिषह को सहन नहीं कर सकता, वह कटिबंध वस्त्र (चोलपट्टा) रख सकता है.
श्री आचारांग सूत्र में कही गई इन्ही बातों के प्रमाण हमें मथुरा जैन स्तूप के पुरातात्विक अवशेषों से मिलते है. जैसे मैंने पहले भी बताया की यह स्तूप से जो अवशेष मिलें हैं वह लगभग १६०० - २२०० वर्ष प्राचीन हैं और तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के साथ-साथ श्रमणों की प्रतिमाएँ (तीर्थंकरों की प्रतिमा के पादपीठ पे या स्तूप के अन्य अवशेषों से) भी प्राप्त हुई है. इन प्रतिमाओं की खास बात यह है कि श्रमणो के हाथों में रजोहरण, मुहपत्ती और पात्र की झोली थी, जिन सब का उपयोग श्वेतांबर श्रमण ही करतें हैं. अगर वस्त्र सम्बन्धी निरिक्षण किया जाए तो तो वे आचारांग सूत्र में दिए गए विवरण से यह अवशेष हूबहू मिलते हैं - मुनिओं की नग्न, एक वस्त्रधारी और दो वस्त्रधारी प्रतिमाएँ हमें देखने मिलती है ! कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना था की यह प्रतिमा दिगंबर संप्रदाय के ऐलक और क्षुल्लक को सूचित करती है जो वस्त्र का उपयोग करते है - परन्तु यहाँ उल्लेखनीय है की पादपीठ में उनकी पदवी मुनि और आचार्य बताई गई है. जैसा की मैंने पहले बताया यह प्रतिमाएं निःशंक श्वेतांबर संप्रदाय की है क्योंकि उपकरणों की समानता के साथ-साथ इन प्रतिमाओं के अभिलेखों में नाम जो अंकित है वह कल्पसूत्र स्थविरावली में मिलतें हैं. इन सब तत्थ्यो से सिद्ध होता है की श्वेतांबर - वस्त्रधारी साधु की परंपरा परिवर्ती कालीन नहीं है जैसा दिगंबर संप्रदाय मानता है. परन्तु यह भी हमें स्वीकार करना होगा की श्वेतांबर संप्रदाय में वस्त्र-पात्र ग्रहण सम्बन्धी आचारो में काफी बदलाव आयें है.
 |
| कंकाली टीला के जैन स्तूप से प्राप्त एक वस्त्र धारी श्वेतांबर जैन श्रमण की प्रतिमा |
 |
| कंकाली टीला के जैन स्तूप से प्राप्त सम्पूर्ण वस्त्र धरी (एकदम बाएं तरफ) और एक वस्त्र धारी श्वेतांबर जैन श्रमणो की प्रतिमाएं |
 |
| कंकाली टीला के जैन स्तूप से प्राप्त निर्वस्त्र जैन श्रमण की प्रतिमा (दाएं तरफ) जिनके हाथ में पात्र की झोली है. बायीं और साध्वीजी की प्रतिमा है जिनके भी हाथ में पात्र है |
 |
| मथुरा के आयगपट्ट पे प्रभु श्री पार्श्वनाथ के दोनों तरफ एक वस्त्र (लंगोट) धारी श्वेताम्बर जैन श्रमण |
~~~~~~~~~~~~~~
C. मूर्तिपूजा का विवाद – जैन धर्म के कुछ उप-संप्रदाय (दिगंबर संप्रदाय के तारणपंथी और श्वेतांबर संप्रदाय के स्थानकवासी और तेरापंथी) मूर्तिपूजा का विरोध करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है मूर्तिपूजा के नाम पे बढ़ता हुआ आडम्बर, हिंसा और कर्मकांड. इस विषय पे मै विशेष चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि -
१. मूर्तिपूजा का विरोध करने वाले सारे उप-संप्रदाय, परिवर्ती कालीन हैं (१५वी -१६वी शताब्दी के बाद इनका उद्भव हुआ है)
२. श्री सूत्रकृतांग सूत्र, श्री उत्तराध्ययन सूत्र (निर्युक्ति), श्री स्थानांग सूत्र, श्री समवायांग सूत्र, श्री भगवती सूत्र, श्री ज्ञाताधर्मकथा आदि अनेक आगमों में मूर्तिपूजा सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते है.
३. पुरातात्विक दृष्टि से प्रभु श्री महावीर के १५० वर्ष पश्चात के समय की प्रतिमाएं आज हमें प्राप्त होती है.
यद्यपि निर्गुणोपासना या भावाराधना एक उच्च स्थिति है, पर आज के युग में यह मात्र कुछ ही महानुभावों के लिए संभव है. आलम्बन बिना आराधना करना एक सामान्य श्रावक के लिए काफी कठिन है. मूर्तिपूजा की आवश्यकता प्राथमिक स्तर पे उसी प्रकार है जिस प्रकार वर्णमाला का अर्थ समझने के लिए चित्रों की सहायता जरुरी है. अधिक क्या, मूर्तिपूजा के विरोधी उपसम्प्रदायों के धर्मगुरुओं की मूर्तियां और पगलिये आज स्थापित करना एक आम बात हो गई है. इन उपसम्प्रदायों के अनुयायिओं के घरों में अपने धर्मगुरुओं के चित्रों को देखा जा सकता है. इसीलिए मूर्तिपूजा का विरोध नहीं करना चाहिए और जो आराधक निर्गुणोपासना द्वारा प्रभु तक पहुंच सकते है उनको मिथ्यात्वी भी नहीं कहना चाहिए.
~~~~~~~~~~~~~~
D. तिथि विवाद - जैसे हमने देखा की अनेक विवादों की वजह से हम इतने सम्प्रदायों-उपसम्प्रदायों और गच्छो में बटें हुए हैं; पर यदि कोई ऐसा विवाद है जिससे एक गच्छ में विभाजन हुआ है तो वह 'पर्वतिथि' के निर्णय को ले कर है. पिछले लगभग १००-१२० साल से श्वेतांबर मूर्तिपूजक संप्रदाय के तपागच्छ में यह विवाद उत्पन्न हुआ है, पर इसकी जड़ें और इतिहास इतना पुराना और पेचीदा है की इस विवाद को समझना मुश्किल बन चूका है. इसीलिए सरल शब्दों में मै इसके इतिहास को समझाने का प्रयत्न करूँगा.
सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं की तिथि क्या होती है. “तिथि” काल के बीच की समयावधि है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच अनुदैर्ध्य-कोण (Longitudinal angle) १२° का एक पूर्णांक है. यानी, चंद्र द्वारा कोणीय दूरी को १२° से बदलने के लिए लिए गए समय को तिथि कहा जाता है. तिथि, दिन में किसी भी समय आरम्भ हो सकती हैं और इसकी अवधि उन्नीस से छब्बीस घंटे तक हो सकती है. जो तिथि, सूर्योदय से पूर्व आरंभ हो जाती है और अगले सूर्योदय के बाद तक रहती है तो उस तिथि की वृद्धि हो जाती है अर्थात् वह “वृद्धि तिथि” कहलाती है लेकिन जो तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ हो और अगले सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो उस तिथि का क्षय हो जाता है अर्थात् वह “क्षय तिथि” कहलाती है. तिथि क्या होती है, वह समझने के बाद अब हम इस विवाद के इतिहास को समझते हैं-
१. महत्वपूर्ण पर्वतिथियां - जैन शास्त्रों में, धर्मकी विशेष आराधना के लिए कुछ दिनों को निर्युक्त किया गया है जिन्हे 'पर्वतिथि' कहा जाता है. श्री महानिशीथ सूत्र में बताया गया है की आगामी जीवनके आयुष्य का बंध विशेष करके काल की पर्वसंधिओ में होने से पर्वतिथिओं की विशेष आराधना करनी चाहिए. श्री सूत्रकृतांग सूत्र में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या को पर्वतिथि बताया गया है और अन्य साहित्य जैसे श्राद्धविधि प्रकरण और सेनप्रश्न में दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा/अमावस्या को पर्वतिथि बताया गया है.
२. जैन आगमिक पंचांग का विच्छेद : जैसे दिनों और तारीखों का परिचय हमें आधुनिक कैलेंडर देता है वैसे ही सामान्य तिथि और पर्वतिथि की जानकारी हमें पंचांग से प्राप्त होती है. श्री चंद्रप्रज्ञप्ति और श्री सूर्यप्रज्ञप्ति जैसे उपांग-आगमों में हमें जैन पंचांग का विवरण प्राप्त होता है जिसे “लोकोत्तर” पंचांग भी कहा जाता था. इस जैन पंचांग में पांच साल के समयचक्र को एक युग कहा जाता था. हर ६१ दिनों में एक तिथि को निकाल दिया जाता था और हर ३० महीनों में एक नया महीना जोड़ा जाता था. इतने खगोलशास्त्र में न उतरते हुए हम अगर इसी बात को सरल शब्दों में समजे तो इस जैन पंचांग का इतना अद्भुत गणित था की तिथि की वृद्धि होती ही नहीं थी. परन्तु काल के प्रवाह में लौकिक (वैदिक) ज्योतिष गणित में फेरफार होने से, लोकोत्तर (जैन) पंचांग और लौकिक (वैदिक) पंचांगों में तिथिओं में [और खास कर के मुख्य पर्वो (जैसे दीवाली/ नव-वर्ष आदि) की तिथिओं में] बहुत अंतर होने लगा. जैन समाज लौकिक वर्ग के साथ जुड़े रहने के लिए आगमिक पंचांग का पालन करना धीरे धीरे छोड़ दिया और प्रभु महावीर के निर्वाण के लगभग ५०० वर्ष पश्चात जैन पंचांग और उसका गणित लुप्त हुआ (और लोकोत्तर पंचांग का विच्छेद हुआ).
३. वैदिक पंचांग को अपनाया जाना- जैन आगमिक पंचांग का लोप होने के बाद भी जैन समाज को अपनी आराधना के लिए एक पंचांग की आवश्यकता तो रही ही - इसलिए पूर्वाचार्यों ने लौकिक (वैदिक/ हिन्दू) पंचांग को अपनाने की स्वीकृति दी. परन्तु इसमें समस्या यह थी की लौकिक-हिंदू पंचांग, सूर्योदय के समय चंद्रमा की स्थिति पर आधारित रहता था और विभिन्न शहरों में अलग-अलग सूर्योदय का समय होने से सभी विस्तारो का पंचांग अलग रहता था -परन्तु भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले जैनो के लिए अलग-अलग पंचांग रखना संभव नहीं था. इसीलिए उस समय के पूर्वाचार्यों ने जोधपुर से निकलने वाले चण्डाशुचंडु वैदिक पंचांग को अपनाया जो पुरे भारतवर्ष के लिए समान रखा गया. जिस जैन पंचांग में उस समय तक तिथिओं की वृद्धि नहीं होती थी, वह चण्डाशुचंडु पंचांग को आधार मानने से शुरू हो गई. विक्रम सम्वत २०१४ (ईस्वी सन १९५८) तक इस पंचांग के आधार पे जैन तिथिओं का निर्णय होता रहा जिसके बाद मुंबई से निकलने वाले जन्मभूमि नाम के वैदिक पंचांग को समस्त तपागच्छ ने एकमत से अपनाया (जिसमे भी तिथिओं की वृद्धि होती है). इस वर्णन से सिद्ध होता है की आज के दिन में प्रकाशित होने वाले कोई भी जैन पंचांग का गणित, प्राचीन आगमों पर आधारित नहीं है.
४. उदित तिथि का सिद्धांत - जैन धर्म की क्रियाएँ तप प्रधान होती है और तप सूर्योदय से प्रारम्भ होता है, इसीलिए सूर्योदय के समय जो तिथि प्रवर्त्तमान होती है (उदित तिथि) उसे पूरे दिन के लिए लागू किया जाता है (भले ही चंद्रमा की स्तिथि सूर्योदय के कुछ समय बाद अगली तीथी में बदल जाए). उदित तिथि की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए "श्राद्धविधिकौमुदी" और "उपदेशकल्पवल्ली" ग्रंथो में यह स्पष्ट उद्घोष है की सूर्योदय के समय में जो तिथि हो उसे ही प्रमाण करनी. दूसरी तिथिओं को प्रमाणित करने से आज्ञाभंग, अनवस्था, मिथ्यात्व और विराधना प्राप्त होती है -
"उदयम्मि जा तिहि सा, पमाणमिअरीई कीरमणीए।
आणाभंगणवत्था-मिच्छत्तविराहणं पावे।।"
परन्तु, यहाँ उल्लेखनीय है की खरतरगच्छ के अनुयायी उदित तिथि के बदले वर्तमान तिथि की आराधना करते है - यानी सूर्योदय के समय भले ही तेरस तिथि हो पर यदि शाम को वह चर्तुर्दशी हो जाती हो तो वह पक्खी प्रतिक्रमण की आराधना उसी दिन करते है (यानी उदित तेरस के दिन ही वर्तमान चतुर्दशी की आराधना करते है) .
C. मूर्तिपूजा का विवाद – जैन धर्म के कुछ उप-संप्रदाय (दिगंबर संप्रदाय के तारणपंथी और श्वेतांबर संप्रदाय के स्थानकवासी और तेरापंथी) मूर्तिपूजा का विरोध करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है मूर्तिपूजा के नाम पे बढ़ता हुआ आडम्बर, हिंसा और कर्मकांड. इस विषय पे मै विशेष चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि -
१. मूर्तिपूजा का विरोध करने वाले सारे उप-संप्रदाय, परिवर्ती कालीन हैं (१५वी -१६वी शताब्दी के बाद इनका उद्भव हुआ है)
२. श्री सूत्रकृतांग सूत्र, श्री उत्तराध्ययन सूत्र (निर्युक्ति), श्री स्थानांग सूत्र, श्री समवायांग सूत्र, श्री भगवती सूत्र, श्री ज्ञाताधर्मकथा आदि अनेक आगमों में मूर्तिपूजा सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते है.
३. पुरातात्विक दृष्टि से प्रभु श्री महावीर के १५० वर्ष पश्चात के समय की प्रतिमाएं आज हमें प्राप्त होती है.
यद्यपि निर्गुणोपासना या भावाराधना एक उच्च स्थिति है, पर आज के युग में यह मात्र कुछ ही महानुभावों के लिए संभव है. आलम्बन बिना आराधना करना एक सामान्य श्रावक के लिए काफी कठिन है. मूर्तिपूजा की आवश्यकता प्राथमिक स्तर पे उसी प्रकार है जिस प्रकार वर्णमाला का अर्थ समझने के लिए चित्रों की सहायता जरुरी है. अधिक क्या, मूर्तिपूजा के विरोधी उपसम्प्रदायों के धर्मगुरुओं की मूर्तियां और पगलिये आज स्थापित करना एक आम बात हो गई है. इन उपसम्प्रदायों के अनुयायिओं के घरों में अपने धर्मगुरुओं के चित्रों को देखा जा सकता है. इसीलिए मूर्तिपूजा का विरोध नहीं करना चाहिए और जो आराधक निर्गुणोपासना द्वारा प्रभु तक पहुंच सकते है उनको मिथ्यात्वी भी नहीं कहना चाहिए.
~~~~~~~~~~~~~~
D. तिथि विवाद - जैसे हमने देखा की अनेक विवादों की वजह से हम इतने सम्प्रदायों-उपसम्प्रदायों और गच्छो में बटें हुए हैं; पर यदि कोई ऐसा विवाद है जिससे एक गच्छ में विभाजन हुआ है तो वह 'पर्वतिथि' के निर्णय को ले कर है. पिछले लगभग १००-१२० साल से श्वेतांबर मूर्तिपूजक संप्रदाय के तपागच्छ में यह विवाद उत्पन्न हुआ है, पर इसकी जड़ें और इतिहास इतना पुराना और पेचीदा है की इस विवाद को समझना मुश्किल बन चूका है. इसीलिए सरल शब्दों में मै इसके इतिहास को समझाने का प्रयत्न करूँगा.
सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं की तिथि क्या होती है. “तिथि” काल के बीच की समयावधि है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच अनुदैर्ध्य-कोण (Longitudinal angle) १२° का एक पूर्णांक है. यानी, चंद्र द्वारा कोणीय दूरी को १२° से बदलने के लिए लिए गए समय को तिथि कहा जाता है. तिथि, दिन में किसी भी समय आरम्भ हो सकती हैं और इसकी अवधि उन्नीस से छब्बीस घंटे तक हो सकती है. जो तिथि, सूर्योदय से पूर्व आरंभ हो जाती है और अगले सूर्योदय के बाद तक रहती है तो उस तिथि की वृद्धि हो जाती है अर्थात् वह “वृद्धि तिथि” कहलाती है लेकिन जो तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ हो और अगले सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो उस तिथि का क्षय हो जाता है अर्थात् वह “क्षय तिथि” कहलाती है. तिथि क्या होती है, वह समझने के बाद अब हम इस विवाद के इतिहास को समझते हैं-
१. महत्वपूर्ण पर्वतिथियां - जैन शास्त्रों में, धर्मकी विशेष आराधना के लिए कुछ दिनों को निर्युक्त किया गया है जिन्हे 'पर्वतिथि' कहा जाता है. श्री महानिशीथ सूत्र में बताया गया है की आगामी जीवनके आयुष्य का बंध विशेष करके काल की पर्वसंधिओ में होने से पर्वतिथिओं की विशेष आराधना करनी चाहिए. श्री सूत्रकृतांग सूत्र में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या को पर्वतिथि बताया गया है और अन्य साहित्य जैसे श्राद्धविधि प्रकरण और सेनप्रश्न में दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा/अमावस्या को पर्वतिथि बताया गया है.
२. जैन आगमिक पंचांग का विच्छेद : जैसे दिनों और तारीखों का परिचय हमें आधुनिक कैलेंडर देता है वैसे ही सामान्य तिथि और पर्वतिथि की जानकारी हमें पंचांग से प्राप्त होती है. श्री चंद्रप्रज्ञप्ति और श्री सूर्यप्रज्ञप्ति जैसे उपांग-आगमों में हमें जैन पंचांग का विवरण प्राप्त होता है जिसे “लोकोत्तर” पंचांग भी कहा जाता था. इस जैन पंचांग में पांच साल के समयचक्र को एक युग कहा जाता था. हर ६१ दिनों में एक तिथि को निकाल दिया जाता था और हर ३० महीनों में एक नया महीना जोड़ा जाता था. इतने खगोलशास्त्र में न उतरते हुए हम अगर इसी बात को सरल शब्दों में समजे तो इस जैन पंचांग का इतना अद्भुत गणित था की तिथि की वृद्धि होती ही नहीं थी. परन्तु काल के प्रवाह में लौकिक (वैदिक) ज्योतिष गणित में फेरफार होने से, लोकोत्तर (जैन) पंचांग और लौकिक (वैदिक) पंचांगों में तिथिओं में [और खास कर के मुख्य पर्वो (जैसे दीवाली/ नव-वर्ष आदि) की तिथिओं में] बहुत अंतर होने लगा. जैन समाज लौकिक वर्ग के साथ जुड़े रहने के लिए आगमिक पंचांग का पालन करना धीरे धीरे छोड़ दिया और प्रभु महावीर के निर्वाण के लगभग ५०० वर्ष पश्चात जैन पंचांग और उसका गणित लुप्त हुआ (और लोकोत्तर पंचांग का विच्छेद हुआ).
३. वैदिक पंचांग को अपनाया जाना- जैन आगमिक पंचांग का लोप होने के बाद भी जैन समाज को अपनी आराधना के लिए एक पंचांग की आवश्यकता तो रही ही - इसलिए पूर्वाचार्यों ने लौकिक (वैदिक/ हिन्दू) पंचांग को अपनाने की स्वीकृति दी. परन्तु इसमें समस्या यह थी की लौकिक-हिंदू पंचांग, सूर्योदय के समय चंद्रमा की स्थिति पर आधारित रहता था और विभिन्न शहरों में अलग-अलग सूर्योदय का समय होने से सभी विस्तारो का पंचांग अलग रहता था -परन्तु भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले जैनो के लिए अलग-अलग पंचांग रखना संभव नहीं था. इसीलिए उस समय के पूर्वाचार्यों ने जोधपुर से निकलने वाले चण्डाशुचंडु वैदिक पंचांग को अपनाया जो पुरे भारतवर्ष के लिए समान रखा गया. जिस जैन पंचांग में उस समय तक तिथिओं की वृद्धि नहीं होती थी, वह चण्डाशुचंडु पंचांग को आधार मानने से शुरू हो गई. विक्रम सम्वत २०१४ (ईस्वी सन १९५८) तक इस पंचांग के आधार पे जैन तिथिओं का निर्णय होता रहा जिसके बाद मुंबई से निकलने वाले जन्मभूमि नाम के वैदिक पंचांग को समस्त तपागच्छ ने एकमत से अपनाया (जिसमे भी तिथिओं की वृद्धि होती है). इस वर्णन से सिद्ध होता है की आज के दिन में प्रकाशित होने वाले कोई भी जैन पंचांग का गणित, प्राचीन आगमों पर आधारित नहीं है.
४. उदित तिथि का सिद्धांत - जैन धर्म की क्रियाएँ तप प्रधान होती है और तप सूर्योदय से प्रारम्भ होता है, इसीलिए सूर्योदय के समय जो तिथि प्रवर्त्तमान होती है (उदित तिथि) उसे पूरे दिन के लिए लागू किया जाता है (भले ही चंद्रमा की स्तिथि सूर्योदय के कुछ समय बाद अगली तीथी में बदल जाए). उदित तिथि की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए "श्राद्धविधिकौमुदी" और "उपदेशकल्पवल्ली" ग्रंथो में यह स्पष्ट उद्घोष है की सूर्योदय के समय में जो तिथि हो उसे ही प्रमाण करनी. दूसरी तिथिओं को प्रमाणित करने से आज्ञाभंग, अनवस्था, मिथ्यात्व और विराधना प्राप्त होती है -
"उदयम्मि जा तिहि सा, पमाणमिअरीई कीरमणीए।
आणाभंगणवत्था-मिच्छत्तविराहणं पावे।।"
परन्तु, यहाँ उल्लेखनीय है की खरतरगच्छ के अनुयायी उदित तिथि के बदले वर्तमान तिथि की आराधना करते है - यानी सूर्योदय के समय भले ही तेरस तिथि हो पर यदि शाम को वह चर्तुर्दशी हो जाती हो तो वह पक्खी प्रतिक्रमण की आराधना उसी दिन करते है (यानी उदित तेरस के दिन ही वर्तमान चतुर्दशी की आराधना करते है) .
५. क्षय-वृद्धि के समय पर्वतिथि की आराधना और विवाद का कारण - जैसे की हमने समजा की (तपागच्छ में) जब तक उदित तिथि प्राप्त होती है तब तक हर तिथि या पर्वतिथि की आराधना उदित तिथि में ही होनी चाहिए. परन्तु सूर्य-चंद्र के गति में भिन्नता के कारण कुछ तिथि २ सूर्योदय को स्पर्श करती है (जिसे वृद्धि तिथि कहा जाता है) और कुछ तिथि एक भी सूर्योदय को स्पर्श नहीं करती (जिसे क्षय तिथि कहा जाता है). इन तिथि के क्षय एवं वृद्धि के प्रसंग में पर्वतिथि की आराधना कैसे करनी चाहिए उसका मार्गदर्शन श्री उमास्वाति महाराज ने अपने इस प्रघोष द्वारा दिया था – "क्षये पूर्वा तिथि : कार्या, वृद्धौ कार्या तथोत्तरा" . इस प्रघोष को सम्पूर्ण तपागच्छ एकमत से स्वीकारता है - परन्तु तपागच्छ के २ वर्ग जिन्हे "एक तिथि" और "बे तिथि" के नामो से जाना जाता है वे इस प्रघोष के शब्दों का अर्थघटन अलग अलग तरीके से करते है; जिसकी वजह से तिथि विवाद उत्पन्न हुए है-
- “एक तिथि” वर्ग का अर्थघटन - (तिथि) क्षय के प्रसंग में पूर्व की तिथि का क्षय करना चाहिए और वृद्धि के प्रसंग में उत्तर तिथिमे आराधना करनी चाहिए. यानी यह वर्ग मानता है की पर्वतिथिओं की क्षय-वृद्धि नहीं करनी चाहिए.
- “बे तिथि” वर्ग का अर्थघटन - (तिथि) क्षय के प्रसंग में पुर्वतिथि आराधनी चाहिए और वृद्धि के प्रसंग में उत्तर तिथि आराधनी चाहिए. यानी यह वर्ग ऐसा मानता है की पर्वतिथिओं की क्षय-वृद्धि करनी चाहिए.
यह दोनों वर्ग अपने पक्ष की मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए अनेक ग्रंथो के सन्दर्भ भी देते हैं, पर मूल बात को तो कोई देखता ही नहीं है – वर्तमान जैन संघ, तिथि का निर्णय जैनेतरो (वैदिको) द्वारा तैयार हुए पंचांग से करता है, और फिर भी आपस में लड़ता है. जब दोनो ही वर्ग, आज के दिन में प्रभु महावीर द्वारा बताये हुए आगमिक (लोकोत्तर) पंचांग के गणित को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर एक दूसरे को मिथ्यात्वी कैसे कह सकते हैं? आगमों के आधार पे यदि हमारा पंचांग तैयार हो जाए तो हमें इन जैनेतरो के पंचांग का आधार नहीं लेना पड़ेगा और तिथि भेद का भी निवारण हो जायगा. तपागच्छ के कुछ साधु आज भी इसके अभ्यास में जुटे हुए हैं. परन्तु जब तक ऐसा पंचांग बन नहीं जाता तब तक मेरी प्रबुद्ध वाचक वर्ग से विनंती है की, जिसे जिस अर्थघटन से तिथि की आराधना करनी है वे करे - पर एक दूसरे के प्रति द्वेष रखे बिना - एक दूसरे को मिथ्यात्वी कहे बिना - क्योंकि आज के दिन में प्रकाशित होने वाले कोई भी जैन पंचांग का गणित, प्राचीन आगमों पर आधारित ही नहीं है.
~~~~~~~~~~~~~~
E. सवंत्सरी के दिन का विवाद : जैन शास्त्रों में पर्युषण को सबसे पवित्र पर्व का दर्जा दिया गया है. उसमे भी सवंत्सरी पर्व की आराधना करने के द्वारा, पुरे वर्ष में किये गए पापो का परायश्चित करने के साथ-साथ विश्व के समस्त जीवो से क्षमायाचना भी मांगनी होती है. यूँ तो पुरे जैन समाज को इस दिन एक साथ मिल कर आराधना करनी चाहिए पर इसमें भी भेदभाव हैं. श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संप्रदाय के तपागच्छ और खरतरगच्छ भादरवा सूद ४ को इस दिन की आराधना करते है और बाकि सारे श्वेतांबर संप्रदाय (स्थानकवासी, तेरापंथी और कुछ मूर्तिपूजक गच्छ) भादरवा सूद ५ को इस दिन की आराधना करते है. इसी वजह से उनके पर्युषण भी एक दिन बाद शुरू होते हैं. इसका कारण समज़ने के लिए भी हमें इतिहास का सहारा लेना होगा -
१. सवंत्सरी के दिन का स्थिरीकरण - श्री कल्पसूत्र के अनुसार केवल संवत्सरी का एक दिन ही पर्युषण कहलाता है. आगमों में निर्देश है की साधु (और साध्वियां) ३०दिनों से अधिक एक स्थान पर नहीं रह सकते - हालांकि चौमासे (बारिश के मौसम) के चार महीनों के दौरान, आषाढ़ सूद १५ से लेकर कार्तिक सूद १५ तक, उन्हें एक ही जगह पर रहना चाहिए ताकि बरसात के दौरान यात्रा में होने वाली हिंसा को कम किया जा सके. प्राचीन समय में, साधुओं को आषाढ़ सूद १५ तक, यानी बारिश के मौसम से पहले ठहरने के लिए एक उपयुक्त निर्दोष स्थान की आवश्यकता होती थी क्योंकि उस समय उपाश्रयों की सुविधा नहीं होती थी. यदि साधुओं को आषाढ़ सूद १५ तक ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं मिल रही हो तो उन्हें ५० दिन की और अनुग्रह अवधि (मुहलत) दी जाती थी. इन ५० दिनों में जैसे ही उन्हें ठहरने का निर्दोष स्थान मिल जाता था तो वह सवंत्सरी प्रतिक्रमण और वार्षिक क्षमापना कर सकते थे. श्री समवायांग सूत्र और श्री निशीथ सूत्र के अनुसार यदि इन ५० दिनों में भी निर्दोष जगह प्राप्त नहीं होती तो साधुओं को ५०वे दिन (यानी भादरवा सूद ५) को एक पेड़ ने निचे सवंत्सरी प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए और इस सिमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. इससे हमें पता चलता है की भादरवा सूद ५ सवंत्सरी प्रतिक्रमण करने एक ही दिन नहीं, परन्तु अंतिम दिन था.
पूरा जैन संघ एकजुट और संगठित हो कर यह आराधना कर पाए इसीलिए पूर्वाचार्यों ने लगभग ७वीं या ८वीं सदी से भादरवा सूद ५ के दिन को ही सवंत्सरी प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया.
२. सवंत्सरी के दिन का बदलाव - श्री निशीथ भाष्य चूर्णी और श्री कल्पसूत्र टिका में हमें इस विषय की जानकारी प्राप्त होती है. प्रभु महावीर के निर्वाण के ९९३ वर्ष पश्चात, यानी लगभग १०वी सदी में श्री कालिकसूरि नाम के महान आचार्य थे. वे उज्जैनी नगरी में चातुर्मास हेतु बिराजमान थे, परन्तु वहां के राजा के विरोध के कारण उन्हें वहां से विहार करके प्रतिष्ठानपुर नगरी जाना पड़ा. प्रतिष्ठानपुर पहुंच के, श्री कालिकसूरि ने वहां के राजा सत्तावाहन को भादरवा सूद ५ के दिन सवंत्सरी प्रतिक्रमण का उपदेश दिया; तब सत्तावाहन राजा ने आचार्यश्री को बताया की उस दिन (यानी भादरवा सूद ५ को) प्रतिष्ठानपुरमें इंद्र महोत्सव मनाया जाता है इसीलिए उन्होंने आग्रह किया की श्री कालिकसूरि भादरवा सूद ६ (यानि एक दिन बाद) सवंत्सरी की आराधना करें. श्री समवायांग सूत्र और श्री निशीथ सूत्र के निर्देशानुसार भादरवा सूद ५ का उल्लंघन संभव नहीं था, इसीलिए राजा की बात रखने के लिए श्री कालिकसूरिने भादरवा सूद ४ को (यानी एक दिन पहले) सवंत्सरी का प्रतिक्रमण किया. इसी परिवर्तन की वजह से मूर्तिपूजको का बहुला वर्ग (तपागच्छ और खरतरगच्छ) आज तक भादरवा सूद ५ की जगह भादरवा सूद ४ के दिन सवंत्सरी की आराधना करता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार २ सवंत्सरी के बिच ३६० तिथियों जे ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए.
३. जब स्थानकवासी और तेरापंथी संप्रदाय उद्भव में आये तब उन्होंने उन्होंने आषाढ़ सूद १५ से ५० वें दिन संवत्सरी करने का फैसला किया जो जैन आगमो की परिभाषा अनुसार अंतिम दिन है. इसलिए एक सामान्य वर्ष में यह संप्रदाय भादरवा सुद ५ को संवत्सरी की आराधना करते हैं.
प्रबुद्ध वाचक वर्ग इसी इतिहास को पढ़ के समझ सकता है की, आगम अनुसार सवंत्सरी की आराधना करने का कोई निश्चित दिन नहीं है. आषाढ़ सूद १५ से ले कर भादरवा सूद ५ के बिच कभी भी सवंत्सरी की आराधना की जा सकती है - बस २ सवंत्सरी के बिच ३६० तिथियों से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए. इसीलिए किसी भी संप्रदाय की मान्यता को इसमें मिथ्यात्वी कहना गलत होगा;
परन्तु, प्राचीन काल की तरह यदि पूरा जैन समाज एक दिन स्थिर करके सवंत्सरी की आराधना करे तो वह पुरे समाज को संगठित करने का कारण बनेगा.
~~~~~~~~~~~~~~
E. सवंत्सरी के दिन का विवाद : जैन शास्त्रों में पर्युषण को सबसे पवित्र पर्व का दर्जा दिया गया है. उसमे भी सवंत्सरी पर्व की आराधना करने के द्वारा, पुरे वर्ष में किये गए पापो का परायश्चित करने के साथ-साथ विश्व के समस्त जीवो से क्षमायाचना भी मांगनी होती है. यूँ तो पुरे जैन समाज को इस दिन एक साथ मिल कर आराधना करनी चाहिए पर इसमें भी भेदभाव हैं. श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संप्रदाय के तपागच्छ और खरतरगच्छ भादरवा सूद ४ को इस दिन की आराधना करते है और बाकि सारे श्वेतांबर संप्रदाय (स्थानकवासी, तेरापंथी और कुछ मूर्तिपूजक गच्छ) भादरवा सूद ५ को इस दिन की आराधना करते है. इसी वजह से उनके पर्युषण भी एक दिन बाद शुरू होते हैं. इसका कारण समज़ने के लिए भी हमें इतिहास का सहारा लेना होगा -
१. सवंत्सरी के दिन का स्थिरीकरण - श्री कल्पसूत्र के अनुसार केवल संवत्सरी का एक दिन ही पर्युषण कहलाता है. आगमों में निर्देश है की साधु (और साध्वियां) ३०दिनों से अधिक एक स्थान पर नहीं रह सकते - हालांकि चौमासे (बारिश के मौसम) के चार महीनों के दौरान, आषाढ़ सूद १५ से लेकर कार्तिक सूद १५ तक, उन्हें एक ही जगह पर रहना चाहिए ताकि बरसात के दौरान यात्रा में होने वाली हिंसा को कम किया जा सके. प्राचीन समय में, साधुओं को आषाढ़ सूद १५ तक, यानी बारिश के मौसम से पहले ठहरने के लिए एक उपयुक्त निर्दोष स्थान की आवश्यकता होती थी क्योंकि उस समय उपाश्रयों की सुविधा नहीं होती थी. यदि साधुओं को आषाढ़ सूद १५ तक ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं मिल रही हो तो उन्हें ५० दिन की और अनुग्रह अवधि (मुहलत) दी जाती थी. इन ५० दिनों में जैसे ही उन्हें ठहरने का निर्दोष स्थान मिल जाता था तो वह सवंत्सरी प्रतिक्रमण और वार्षिक क्षमापना कर सकते थे. श्री समवायांग सूत्र और श्री निशीथ सूत्र के अनुसार यदि इन ५० दिनों में भी निर्दोष जगह प्राप्त नहीं होती तो साधुओं को ५०वे दिन (यानी भादरवा सूद ५) को एक पेड़ ने निचे सवंत्सरी प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए और इस सिमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. इससे हमें पता चलता है की भादरवा सूद ५ सवंत्सरी प्रतिक्रमण करने एक ही दिन नहीं, परन्तु अंतिम दिन था.
पूरा जैन संघ एकजुट और संगठित हो कर यह आराधना कर पाए इसीलिए पूर्वाचार्यों ने लगभग ७वीं या ८वीं सदी से भादरवा सूद ५ के दिन को ही सवंत्सरी प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया.
२. सवंत्सरी के दिन का बदलाव - श्री निशीथ भाष्य चूर्णी और श्री कल्पसूत्र टिका में हमें इस विषय की जानकारी प्राप्त होती है. प्रभु महावीर के निर्वाण के ९९३ वर्ष पश्चात, यानी लगभग १०वी सदी में श्री कालिकसूरि नाम के महान आचार्य थे. वे उज्जैनी नगरी में चातुर्मास हेतु बिराजमान थे, परन्तु वहां के राजा के विरोध के कारण उन्हें वहां से विहार करके प्रतिष्ठानपुर नगरी जाना पड़ा. प्रतिष्ठानपुर पहुंच के, श्री कालिकसूरि ने वहां के राजा सत्तावाहन को भादरवा सूद ५ के दिन सवंत्सरी प्रतिक्रमण का उपदेश दिया; तब सत्तावाहन राजा ने आचार्यश्री को बताया की उस दिन (यानी भादरवा सूद ५ को) प्रतिष्ठानपुरमें इंद्र महोत्सव मनाया जाता है इसीलिए उन्होंने आग्रह किया की श्री कालिकसूरि भादरवा सूद ६ (यानि एक दिन बाद) सवंत्सरी की आराधना करें. श्री समवायांग सूत्र और श्री निशीथ सूत्र के निर्देशानुसार भादरवा सूद ५ का उल्लंघन संभव नहीं था, इसीलिए राजा की बात रखने के लिए श्री कालिकसूरिने भादरवा सूद ४ को (यानी एक दिन पहले) सवंत्सरी का प्रतिक्रमण किया. इसी परिवर्तन की वजह से मूर्तिपूजको का बहुला वर्ग (तपागच्छ और खरतरगच्छ) आज तक भादरवा सूद ५ की जगह भादरवा सूद ४ के दिन सवंत्सरी की आराधना करता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार २ सवंत्सरी के बिच ३६० तिथियों जे ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए.
३. जब स्थानकवासी और तेरापंथी संप्रदाय उद्भव में आये तब उन्होंने उन्होंने आषाढ़ सूद १५ से ५० वें दिन संवत्सरी करने का फैसला किया जो जैन आगमो की परिभाषा अनुसार अंतिम दिन है. इसलिए एक सामान्य वर्ष में यह संप्रदाय भादरवा सुद ५ को संवत्सरी की आराधना करते हैं.
प्रबुद्ध वाचक वर्ग इसी इतिहास को पढ़ के समझ सकता है की, आगम अनुसार सवंत्सरी की आराधना करने का कोई निश्चित दिन नहीं है. आषाढ़ सूद १५ से ले कर भादरवा सूद ५ के बिच कभी भी सवंत्सरी की आराधना की जा सकती है - बस २ सवंत्सरी के बिच ३६० तिथियों से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए. इसीलिए किसी भी संप्रदाय की मान्यता को इसमें मिथ्यात्वी कहना गलत होगा;
परन्तु, प्राचीन काल की तरह यदि पूरा जैन समाज एक दिन स्थिर करके सवंत्सरी की आराधना करे तो वह पुरे समाज को संगठित करने का कारण बनेगा.
अभी तक चर्चित इन सारे विवादों को छोड़ के भी जैन धर्म में और भी कई विषयों में प्रश्नचिह्न लगे हुए हैं - स्त्रीमुक्ति का प्रश्न, केवली आहार का प्रश्न, मुखवस्त्रीका (मुँहपत्ती) का प्रश्न, नवांगी गुरुपूजा का प्रश्न आदि. यह सारे विवाद उपरोक्त दिए गए विवादों से कम चर्चित है इसीलिए इनके विषय में लिख के इस लेख को और बड़ा नहीं बना रहा हूँ. पर मेरी यही आशा है की कोई भी विवाद की वजह से किसी संप्रदाय पे द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए - "मै सच्चा और बाकि सब गलत", यह बात ज़हन में आते ही हम प्रभु महावीर के वचनो से बहोत दूर चले जाते हैं.
आजकल एक श्लोक काफी चर्चा में है - "तमेव सच्चं निःसंकं जं जिणेहिं पवेइअं"; अर्थात् वही सत्य है और शंका रहित है जो जिनेश्वर (श्री अरिहंत प्रभु) ने फ़रमाया है. प्रबुद्ध वाचक वर्ग से मेरी भी यही विनंती है की इस श्लोक की गहराई तक जाये और प्रभु की वाणी का अध्ययन करे - क्योंकि वही अंतिम सत्य है. यदि आज हम अनेकांतवाद के सिद्धांत को नहीं स्वीकारते तो इसका यही अर्थ निकलता है की हम प्रभु की बात को अंतिम सत्य नहीं मान रहे - हम किसी और की बातों (चाहे वह कोई संप्रदाय हो या कोई धर्मगुरु हो) अंतिम सत्य मान रहे है.
प्रस्तुत लेखन का मेरा एकमात्र उद्देश्य, धर्मभीरु वाचक वर्ग को धर्म और सिद्धांत के नाम पर प्रचलित कुछ मान्यताओं का निष्पक्ष स्वरूप समझाना था, ताकि सम्प्रदायवाद के नाम पे चल रही कड़वाहट थोड़ी कम हो. हो सकता है इस लेख को पढ़ने के बाद आप मुझे "सुधारकवाद" कहो या "उत्सूत्र प्ररूपणा" करने वाला समजो पर इस लेख के द्वारा किसी भी जैन संप्रदाय का न मुझे खंडन करना है न मंडन. संभव है की भावनाओं के प्रवाह में कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी लिखा गया हो तो मै हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ. यदि मुज़से कुछ कटुतियाँ रह गई हो तो मुझे बताएं - मैं उन्हें सुधारने की अवश्य कोशिश करूँगा. इस लेख का अंत मैं एक श्लोक के द्वारा करना चाहूंगा जो मैंने अनेकांतवाद की किसी पुस्तकमे पढ़ा था -
"स्याद्वादो वर्ततेऽस्मिन, पक्षपातो न विद्यते।
नासत्यन्य पीडनं किञ्चित् जैनधर्म: स उच्यते ।।"
आजकल एक श्लोक काफी चर्चा में है - "तमेव सच्चं निःसंकं जं जिणेहिं पवेइअं"; अर्थात् वही सत्य है और शंका रहित है जो जिनेश्वर (श्री अरिहंत प्रभु) ने फ़रमाया है. प्रबुद्ध वाचक वर्ग से मेरी भी यही विनंती है की इस श्लोक की गहराई तक जाये और प्रभु की वाणी का अध्ययन करे - क्योंकि वही अंतिम सत्य है. यदि आज हम अनेकांतवाद के सिद्धांत को नहीं स्वीकारते तो इसका यही अर्थ निकलता है की हम प्रभु की बात को अंतिम सत्य नहीं मान रहे - हम किसी और की बातों (चाहे वह कोई संप्रदाय हो या कोई धर्मगुरु हो) अंतिम सत्य मान रहे है.
प्रस्तुत लेखन का मेरा एकमात्र उद्देश्य, धर्मभीरु वाचक वर्ग को धर्म और सिद्धांत के नाम पर प्रचलित कुछ मान्यताओं का निष्पक्ष स्वरूप समझाना था, ताकि सम्प्रदायवाद के नाम पे चल रही कड़वाहट थोड़ी कम हो. हो सकता है इस लेख को पढ़ने के बाद आप मुझे "सुधारकवाद" कहो या "उत्सूत्र प्ररूपणा" करने वाला समजो पर इस लेख के द्वारा किसी भी जैन संप्रदाय का न मुझे खंडन करना है न मंडन. संभव है की भावनाओं के प्रवाह में कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी लिखा गया हो तो मै हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ. यदि मुज़से कुछ कटुतियाँ रह गई हो तो मुझे बताएं - मैं उन्हें सुधारने की अवश्य कोशिश करूँगा. इस लेख का अंत मैं एक श्लोक के द्वारा करना चाहूंगा जो मैंने अनेकांतवाद की किसी पुस्तकमे पढ़ा था -
"स्याद्वादो वर्ततेऽस्मिन, पक्षपातो न विद्यते।
नासत्यन्य पीडनं किञ्चित् जैनधर्म: स उच्यते ।।"
जो स्याद्वाद में आस्था रखता है तथा पक्षपात से दूर है और जो किसीको पीड़ा नहीं देता, वही जैन धर्म का सच्चा अनुयायी है.








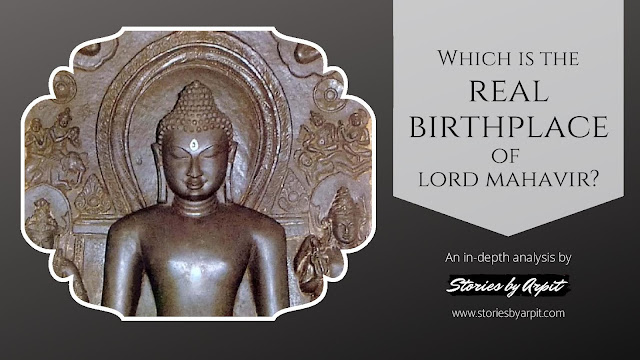








Really nice article with plenty of research work and I too would love to see if some hatred amongst different sects of jains lessen through it. On many points I do differ with you for which we shall speak some day later as above all ultimate aim should be to defeat underlying hatred amongst different sects of jains.
ReplyDeleteDear Samir bhai,
DeleteWould surely love to understand your observations :)
Very well compiled with so much information.. thanks for sharing..
ReplyDeleteGlad you found it informative :)
DeleteArpit very well written hats off you need guts for that deep research 🙏
ReplyDeleteThank you so much :)
DeleteFrom where do you find such beautiful, non-pixelated and refined images. The pics from Kankali Tila are awesome! Seems you are great with camera skills. In Jinprabhasuriji's Vividh Tirth Kalpa (written during Khilji's reign) Mathura Dev Nimmitta Stupa finds a special mention. The Suriji after personal visit to the place wrote that the Stupa premises was freed from Digambar hold by Prabhavak Acharya Shri Bappabhattasuriji. Most of the naked kayotsarg idols are from 5th or 6th century AD. So can it be the case that they were a later edition post Digamber occupation? The iconographic features of kayotsarg idols are pretty basic and defy even murti mandan norms - the padmasana idols were more exquisitively carved. Why this difference? Why red sandstone was used when prior to Kushan era Mauryans used marble and had mastered murti making art as evident in Samrat Samprati Kalin idols? The stupa was made by Kubera Devi in the Shashan of Shri Suparshvanathji and then was covered with stones to protect from greedy people post Shri Parshavanathji's era (prayah). So as we see in today's temples, the outer wall sculptures are of sandstone and less in finace compared to the ones installed in the sanctum sanctorum. Interestingly, Kankali Mound excavations yielded the ruins of stupa and one Shwetamber and Digamber temple ruins. A sixty year old Jain Satya Prakash article carries pics of two tirthankar idols recovered from Shwetamber side of the stupa ruins. Sadly, the pics are blackened. If you have pics of idols recovered from Kankali Tila can you please share? The queries I posed were bugging me since a long time. Your post provideed a platform to articulate them. Thanks for that! Hope to find answers soon:)
ReplyDeletePlease read it as "less in finesse" - typo!
DeleteThe Kankali tila idols have not been clicked by me :) They have either been sourced from various publications or from Wikimedia Commons. The naked karyotsarg idols predate 2nd CE, not post 5th CE and were commonly worshipped by both the Digambars and Shwetambars.
DeleteThe Mauryans never used marble - polished stone was used. The idols which are commonly known as Samprati Kalin are actually installed post the Gupta age (5 CE)
I would like to request you to read some of my articles below -
http://www.storiesbyarpit.com/2018/09/the-untold-story-of-jainism-3000-year.html
http://www.storiesbyarpit.com/2019/08/sculpting-tirthankars-q-on-jain.html
With regards to the idols appearing in Satyaprakash magazine, sadly I too dont have the pictures.
Very well compiled...lot of effort has gone down...people will feel controversial...but need to read it not once .......best part...in Hindi...i will read it once more then will raise few questions..to get clarity...
ReplyDeleteDear Sir,
DeleteThank you. Glad you found it informative. Would surely love to understand your questions as well :)
Really a great research and superb writing which makes us understand the real Jain Dharma. Really appreciated. The only thing I would like to tell you is that we are not able to make a print and make people read as many people don't read on mobiles or in emails. So if there is any way that we can take a print out or can subscribe in which we can have a print out then it will hr people to understand. Even we can ask our guru महाराज to read and then make us more enlightened
ReplyDeleteThank you. The blog is in a printable format. If you are using any of the browsers like Google Chrome, Firefox or IE then you can print by pressing Ctrl+P
DeleteHi Arpit Upadhyay Amar Muni and Acharya Sushil Muni had similar thoughts on the divisions in Jainism. Both of them sthanakwasis also built temples containing both digambar and swetamber idols. Sookti triveni written by Amar Muni Ji is one of the best books on Indian philosophy he believed that sanatan dharma(Hinduism Buddhism and Jainism) can't be understood without each other.
ReplyDeleteAgree. I am also deeply influenced by Upadhyay Shri Amar muni's books
DeleteHey Arpit a very rare book by Amar Muni ji Sookti Triveni is available with me if you wish to read it let me know I know you are in Kolkata too contact me on rkhajanchi14@gmail.com. Very few copies of Sookti Triveni were published because this book is of very high spiritual content and not many people would be able to understand it.
DeleteSure Rushil,
DeleteI would love to read it. Will surely contact you once this lockdown ends
Arpit,
ReplyDeleteVery well researched and compiled. I compliment you on the time and effort you dedicated to jain scriptures and glean the essense. Salute to your bhakti to jain dharm.
Thank you so much.
DeleteIt was indeed an eye opener for all those believing in their superiority among other sects!
ReplyDeleteI will surely share this as much as I can to make them understand the true meaning of jainism!
Thank you very much Mr. Arpit, for providing such rare information!
Glad you found it informative !
DeleteHi Arpit,
ReplyDeleteThank you for this very informative and well organised article. Provides clear understanding of issues. I always believed in underlying theme here - follow as one believes but do not have hatred for others. You have put it clearly enough. But above that I learned one more thing that we should strive to find truth as well that will make us true Jain.
True :) Hope we delve deeper and try to reveal the truth !
Deleteविवाद के सभी पहलुओं पर समुचित प्रकाश डालते हुए आपने बहुत ही अच्छा लेख लिखा है।आपसी वैमनस्यता अपनी मत के प्रति आग्रह अन्य नेताओं के प्रति दुराग्रह का अनादर कम करने में व सांप्रदायिक सौहार्द्र को बढ़ाने में आपका लेख बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। पूरा लेखा दे उपांत पढ़ने के पश्चात ज्ञात होता है कि आपने बहुत समय लगाकर बहुत मेहनत व बहुत अध्ययन करके यह शोध पत्र लिखा है।आपके द्वारा जो भावनाएं इस पत्र के माध्यम से व्यक्ति की गई है यदि उन्हें समाज समझ ले तो जैन धर्म का बहुत उत्थान हो सकता है।
ReplyDeleteआपका खूब खूब आभार ! हो सके तो इस लेख को सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग तक पहुंचाए.
Deleteआपने लेख अथक प्रयास से और सभी पहलू ओंको ध्यानमें रखते हुए लिखा है l ज्यादा तर लोग अनेकान्तवाद के गुण तो गाते है। पर आचरण में नही लाते ,वास्तविकता तो यह है कि लोग संप्रदारसे अलग होना नही चाहते ।इासिमें अनेकान्त को भूला देते है I आपकी सोच बहुत अच्छी है । सांप्रदायिकतामें भगवान को ना बांटे ,यही तो धर्मकी समझ है I
ReplyDeleteआपका खूब खूब आभार ! हो सके तो इस लेख को समाज के प्रबुद्ध वर्ग तक पहुंचाए.
Deleteआप के लेख मेने आज से ही पडने चालु किये , आप अपने लेख को पुरे समाधान के साथ लिखते है , जो कॉफी अच्छा है 👍💐
DeleteHey Arpit I've been reading your articles recently. I appreciate your effort and bringing such topics to our attention. But to be honest to me it seems more of Shwetambar perspective. There's little lack Jain digambara sects perspective here. There's already Monksa much gap of understanding, I don't want you to ruin your noble efforts by supporting sectarian perspectives here. Also i want to inform that, thode monks on statues of kankali tila are also considered Ailak and kshullakas of digambara sect and such monks and nuns with one/two clothes still exist in digambara sangha till date. Even other historians called them Ajivikas. Almost similar legends of devi declaring temple belonging to digambara sect is mentioned in equally old other scriptures. It's difficult to say whos right again. Painful part is you mentioned removing of chakshu with iron rods let me tell you there are more worse stuffs done to digambara jain statues in the past to convert them to shwetambar and to occupy temples forcibly, monetarily and even politically which was never needed if according to you Shwetambar monks was okay reverring digambara attire.
ReplyDeleteI dont know whos right but i want you to understand that on many statues no sign of even a loin cloth was ever there and was just carved later out of "least requirement". I understand you're not handling sectarian agenda here but for me it looked like you just justified some hypothetical sectarian beliefs and wrongly put them as facts.
Dear Atulji,
DeleteThank you for taking out time and absorbing the post. I would like to clarify upfront that I have not justified any hypothetical sectarian beliefs and wrongly put them as facts. What I have said, is based only on the facts.
I just want to add that the monks depicted on Kankali tila sculptures are not Ailaks and Kshullaks but Acharyas and Munis. The names on the pedestals show their designation as well as their affiliations of Kula-Gana-Shakha which match exactly with the Kalpasutra Sthaviravali, which is a Shwetambar Sect. Infact 2 of the idols have inscriptions stating - "Shwetambar Mula Sangha" and "Shwetambar Mathuri Sangha"
Even I have repeated the Girnar story here not to prove the superiority of a sect over other - I mentioned it here to show that earlier both the sects shared the same temple and the reason why the Shwetambar traditon started carving Katisutra - Kandora.
In this article I have not justified who is right or who is wrong. The sole reason I wrote this was to remove the underlying hatred between all sects.
Correction: Dear Atulji,
DeleteThank you for taking out time and absorbing the post. I would like to clarify upfront that I have not justified any hypothetical sectarian beliefs and wrongly put them as facts. What I have said, is based only on the facts.
I just want to add that the monks depicted on Kankali tila sculptures are not Ailaks and Kshullaks but Acharyas and Munis. The names on the pedestals show their designation as well as their affiliations of Kula-Gana-Shakha which match exactly with the Kalpasutra Sthaviravali, which is a text of the Shwetambar Sect. Infact 2 of the idols have inscriptions stating - "Shwetambar Mula Sangha" and "Shwetambar Mathuri Sangha"
Even I have repeated the Girnar story here not to prove the superiority of a sect over other - I mentioned it here to show that earlier both the sects shared the same temple and the reason why the Shwetambar traditon started carving Katisutra - Kandora.
In this article I have not justified who is right or who is wrong. The sole reason I wrote this was to remove the underlying hatred between all sects.
Hi Arpit,
ReplyDeleteHi,
After a very long time, I come across your blog. I really appreciate your efforts and sincere work for it. hats off for this.
It is really very nice article and I wish such article will read by many of us.
In Present times, we forget Definition of “Dharma”. As you rightly mentioned we diverted away from our basics and that is Anekantvad. When you asked any small children of our community he or she knows basic rituals followed in their homes but none of knows about Anekantvad. We mistakenly taken ritual as Dharma.
We all know that any child studying in 9th standard of any schools, considered as 9th standard students. that's way we follow any sampraday, but we must know anyone from his or her level of Aatmic Growth.
In Today's world most of our non Jain freinds knows Jainism means - no onion no garlic, doing fasting and keeping either yellow tilak or wear white cloths over mouth, remain naked etc.....
we are also feels proud in saying how many fasting done, how much we sticking in doing Puja and samayik but no one knows our real treasure of knowledge - Such as Anekantvad, Theory of Karmas etc.
when any one goes deeper in our religion in any area, I surely believes he can find answers of all his questions. it is like google - you can find all answer of every aspect of your life with logical explanation.
we are forgetting real diamonds and fighting for its box.
Hi Arpit. Thank you for putting together this informative and eye opening content. This really explains how far we have moved from the teachings of tirthankars. Thanks again for such wonderful articles.
ReplyDeleteभाई अर्पित जी सविनम्र प्रणाम ।
ReplyDeleteआपकी भावना , उद्देश्यपरक आलेखन सराहनीय है। गहन अध्ययन की स्पष्ट झलक आपके विवेचन में है ।
जिनत्व का मूल तो राग द्वेष , कषाय विकार से मुक्त होने समता समभाव की साधना ही है । जिन धर्म निज कल्याण का मार्ग है । वर्तमान समय के साधनों के बीच युवा पीढ़ी व नई पीढ़ी के जीवन की जो चुनौतीयां है व जो दशा है चाहे stress, anxiety , sadness, depression , addiction इन जैसी सब सारी ही समस्याओं की ओर आज संघ ,समाज के हर मंच पर विचार किया जाना चाहिए।
और अत्यंत ही हर्ष की बात है कि हमारा जिन धर्म जो मूलतः पूर्ण अध्यात्म ध्यान समाधि का मार्ग है इसके वर्तमान की भाषा में सरलीकृत एवं परिष्कृत सत्य साधना ध्यान इन सबके सशक्त समाधान के रुप में उभर कर आई है। सत्य साधना के दस दिवसीय मौन ध्यान शिविर जैनाचार्य श्रीपूज्य श्रीजिनचन्द्रसूरि जी महाराज साहब की प्रेरणा व मार्गदर्शन में कुशलायतन ,नाल बीकानेर राजस्थान व सत्य साधना केन्द्र खैयादा कोलकाता में नियमित हो रहे हैं। यह साधना आत्म शुद्धि के साथ जीवन को संतुलित व संयमित बनाने की पूर्णतः वैज्ञानिक practical विधि है । यथार्थ के धरातल पर धर्म को आत्मसात कर सम्यक् विकास कि दिशा देने में उत्सुक हरेक जन के लिए यह लाभकारी है ।
पुनश्च आपके प्रयास को नमन अभिनंदन
सुनील डागा , इन्दौर
Aap sahi ya galat muje nahi pata.
ReplyDeleteJo jain dharm kheta hai ki hum anekanth waad mai maante hai.wo hi jain aaj khud ke alag alag concepts leke beta hai. Shishyo ko gumrah kar rahe hai. Mai bhi sabhi sadhu ko ek maanta hu.
Aapne khub achcha kaam kiya,
I Just heartily wish that pura jain ek ho jaye. Sab Ki maanyata ko leke...
Guru bhagwant khete hai raag duesh nahi karna. Lekin wakai mai guru bhagwant isko acharan mai le rahe hai...
Digamber sampradai ka Vivaran nahi kiya aapne. Aur 2 gach ke alava aur bhi unka bhi nahi kiya
ReplyDeletevery good artical
ReplyDeleteHello Arpit,
ReplyDeleteLots of research and important information.
I'll try my best to make all jains to be united with my efforts !!!
Very nice and we'll researched article.
ReplyDeleteDude, you are a gem in Jain kul. May ma saraswati bless you further. Your views, study and thoughts are fascinating. And in fact reinstates what is sidelined in this pancham aara.
ReplyDeleteबहुत ही धन्यवाद अर्पित जी ऐसे सुंदर लेख के लिए।
ReplyDeleteजिस धर्म ने पूरे विश्व को अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया आज उसी धर्मों में अनेकांतवाद की दरकार किए बिना लोग अपने अपने मत मतंतर में खो गए हैं
ज्यादातर चर्चा कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे क्रियाएं करनी चाहिए उसी की रहती है और हमारा पक्ष दूसरे से कितना अच्छा है उसी की बातें होती रहती है सिद्धांतों की चर्चा तो कहीं दिख ही नहीं रही खास करके गुजरात में
जिस दिन एक पंथ की संवत्सरी होती है उस दिन दूसरे पंथ वाला बंदा बिल्कुल आराम से अपनी दिनचर्या करता है तो कभी दिमाग में आता है कि मैं जिस पंथ में या संप्रदाय में हूं उनकी बात सही है कि दूसरे पंथ की
जो ज्ञानी जन हमें समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं वह क्या कभी भी एक दूसरे संप्रदाय के साधु साध्वी जी से मिलकर बात भी कर पाते हैं ? साथ रहने की तो बात ही दूर है?
जब कोई धर्म या व्यक्ति या कोई भी सिस्टम, अपने सिद्धांतों से दूर चला जाता है तब यही हालत होती है
हम हमसे बड़ों को तो इस मत मत आंतर से दूर नहीं कर पाएंगे लेकिन आज हर किसी को एक नियम लेना चाहिए कि हम हमारे बच्चों में इस चीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो आगे चलके 40 50 साल में हम इस चीज से ऊपर उठ पाएंगे
सबसे ज्यादा मुश्किल है जब दो संप्रदायों वालों के बीच में विवाह होता है और फिर आपस में जो टकराव चालू होता है तब लगता है कि हम महावीर के अनुयाई है या किसी और के ?
अपने बच्चों को सिद्धांत की बात सिखाओ ।
कौन से संप्रदाय में जाना है उसका चयन उसके ऊपर छोड़ दो